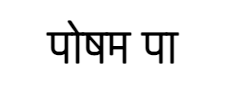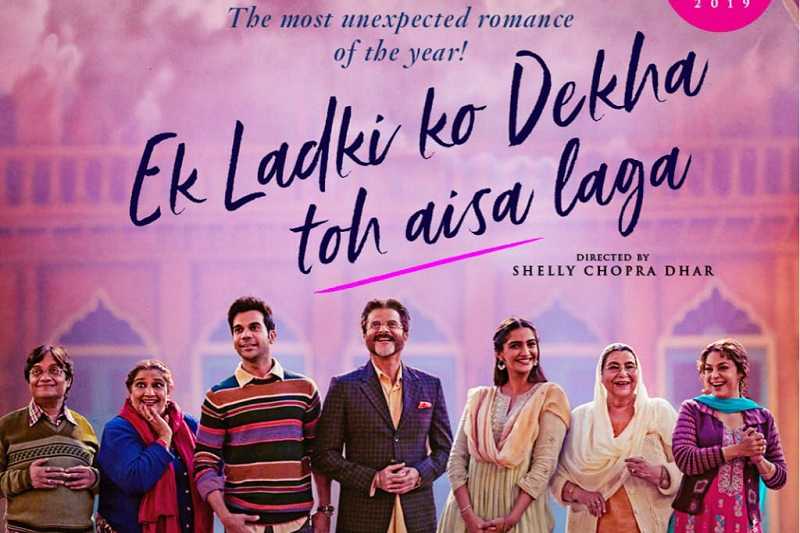भारतीय सिनेमा एक स्तर पर, एक अरसे तक अव्यवहारिक प्रेम, पितृसत्तात्मक सड़े-गले मूल्य और छिछली नाटकीयता का सिनेमा रहा है। आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांध सकते। हालांकि बीच-बीच में कुछ फिल्में इस ढर्रे को तोड़कर सुकून की आहें ज़रूर देती रहती हैं। हफ्ते में एक फ़िल्म ऐसी आ जाती है जिसे ‘ignorance is bliss’ का हिजाब उठाकर देखा जा सकता है। गए हफ्ते की मेरे लिए ऐसी फिल्म ‘102 नॉट आउट’ रही।
ट्रेलर देखकर जिस हल्की-फुल्की, क्यूट कहानी की उम्मीद लगाई थी वो तो पूरी हुई ही, साथ ही सुखद आश्चर्य था फ़िल्म का एक ऐसे विषय का तार छेड़ना जिसे हम बहुत अलग सुरों में सुनने के आदी हैं। और वह विषय है भारतीय समाज में बुढ़ापा।
दत्तात्रेय वखारिया (अमिताभ बच्चन) 102 साल के युवा हैं जिनकी ज़िन्दगी की फिक्रें मानो बालों के कालेपन के साथ जाती रहीं। वे खूब हंसते, कूदते, नाचते हैं। जिस लाचारी, निर्भरता, उदासी के परिप्रेक्ष्य से हम बुढ़ापे को देखते आये हैं, दत्तात्रेय उससे ठीक उलटी दिशा में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ, सामने से आते दिखते हैं उनके सुपुत्र बाबूलाल दत्तात्रेय (ऋषि कपूर) जो कि 75 साल के एक गूढ़ और गंभीर वृद्ध हैं। बाबूलाल घड़ी-घड़ी खुद को याद दिलाते हैं कि अब उनके जीवन में केवल एक इंतज़ार शेष बचा है। वह इंतज़ार जिसकी शुरुआत पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के पूर्ण होने के साथ होती है और जिसका अंत जीवन के अंत के साथ ही होता है। उनके जीवन से नीरसता का बादल किसी समय नहीं छंटता। दीवारों पर रिमाइंडर स्टीकर चिपके हैं और खुद पुरानी यादों की चादरों से।
दत्तात्रेय वखारिया नहीं चाहते कि उनका बेटा जीवन के आखिरी पड़ाव के उस पार उदास आँखों से देखे। वे एक नाटकीय ढंग से अपना फैसला सुनाते हैं कि अगर बाबूलाल ने इस गंभीरता का चोगा न उतार फेंका तो वे उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देंगे। कहते हैं कि मुझे अभी और जीना है, बल्कि जीने की उम्र का रिकॉर्ड तोड़ना है, इसलिए मुझे अपने आसपास नीरस, थके और नेगेटिव लोग नहीं चाहिए और यदि बाबूलाल को उनके साथ इस घर में रहना है तो बाबूलाल को उनकी कही सारी बातें माननी होंगी।
एक बेहद मनोरंजक सीक्वेंस में दत्तात्रेय बाबूलाल से बहुत बचकानी दिखने वाली चीज़ें करवाते हैं। इनमें से एक चीज़ है अपनी उस पुरानी चादर को काट देना जिसके बिना बाबूलाल कभी सोते नहीं। यूँ यह बहुत मामूली चीज़ मालूम होती है मगर इसके मायने जीवन में उतार लेने चाहिए। हम अक्सर ही कुछ लोगों, कुछ चीज़ों, कुछ यादों को अपने इतने करीब कर लेते हैं कि उनसे बिछड़ना जीवन के खत्म होने जैसा हो जाता है। भारतीय परिवेश और इस फ़िल्म की नज़र से देखें तो ये लोग अक्सर हमारी संतानें होती हैं।
भारत का एक आम नागरिक अक्सर अपनी सारी ज़िन्दगी एक सर्वाइवल के लिए लड़ता रहता है, कभी कोई शौक या पैशन सहेजने की फुरसत नहीं कर पाता, अपना प्रोविडेंड फण्ड अपने बच्चों की जायज़ या नाजायज़ माँगों पर लुटा दिया करता है, और अंत में उसके पास जीवन की पूँजी के रूप में कुछ बचता है तो केवल उसकी संतानें। रिटायर होने के बाद भी बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे और उनके लिए सारी सहूलियतें जुटा देना ही उसका उद्देश्य रहता है।
यह फ़िल्म माँ-बाप का बच्चों से यह जो अत्यधिक मोह है, उसपर सवाल करती है। पूछती है कि ऐसे बच्चे जो कभी एक मुस्कान का कारण तक नहीं बने, उन्हें क्यों केवल अपनी असफलता मानकर जीवन भर उसपर शोक करते रहें? क्यों अपनी ही परवरिश में कमियाँ ढूँढते रहें और कोशिश करते रहें उनके अनुसार खुद को ढालने की? क्यों राजा बनकर अपनी जान इस वीभत्स तोते में डाल दी जाए? एक इंसान के रूप में जो इतनी सुन्दर ज़िन्दगी मिली है, उसे अपने लिए जीना क्यों न सीखा जाए?
न केवल यह, फ़िल्म यह भी दिखती है कि बुढ़ापे को अपनी एक कमजोरी के रूप में स्वीकार लेना भी कितना गलत है। बीमारियों को जीवन का हिस्सा और दबे पाँव आते अंत को अपना भाग्य मान लेना इस जीवन का अपमान है और यह करना हमसे वे सभी लम्हें छीन लेता है जो अन्यथा बेहद खूबसूरत और जीवंत हो सकते हैं।
‘102 नॉट आउट’ ये सभी गंभीर बातें एक बाप-बेटे की मीठी नोक-झोंको में कह देती है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के गुजराती लहज़े को छोड़ फिल्म में सभी दृश्य, गीत, व संवाद सहज दिखाई पड़ते हैं। एक-आध मसालेदार मोनोलॉग भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर डाले गए हैं, मगर इतना तो स्वीकार किया जा सकता है।
संगीत भी अच्छा है। और मुम्बई की सभी लोकेशन सजीव हैं। परिवार के साथ देखे जाने के लिए उमेश शुक्ला जी ने एक बेहतरीन फ़िल्म प्रस्तुत की है। इसको देखें और इसके बाद अपने घर के बुज़ुर्गों को कस के गले लगाएं। जीवन के इतने वर्ष सर्वाइव कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
■■■