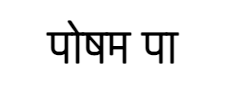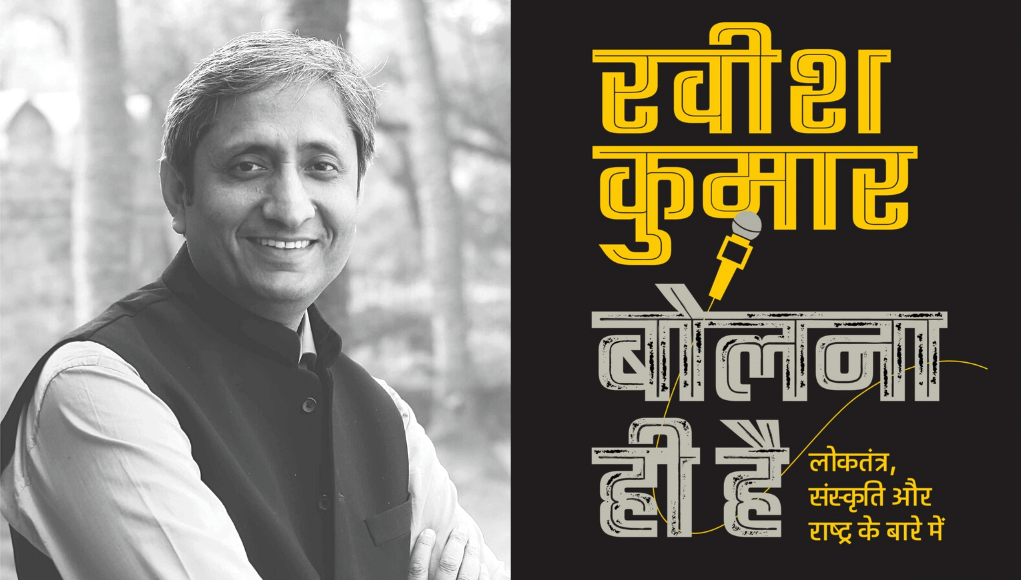रवीश कुमार की किताब ‘बोलना ही है’ से
हर कोई इश्क़ में नहीं होता है और न हर किसी में इश्क़ करने का साहस होता है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग कल्पनाओं में इश्क़ करते हैं। मुझे बाक़ी मुल्कों का पता नहीं, लेकिन भारत में इश्क़ करना अनगिनत सामाजिक-धार्मिक धारणाओं से जंग लड़ना होता है। मोहब्बत हमारे घरों के भीतर प्रतिबन्धित विषय है। कितने माँ-बाप अपने बच्चों से पूछते होंगे कि तुम्हारे जीवन में कोई है? तुम्हें कोई अच्छा लगता है या तुम किसी को चाहती हो? बहुत कम। इतनी कम सामाजिक स्वीकार्यता के बीच किसी से इश्क़ करना, सिर्फ़ ‘आई लव यू’ कहना नहीं होता है।
सबके जीवन में प्रेम की कल्पना फ़िल्मों से आती है। फ़िल्में हमारी दीवानगी की शिल्पकार हैं। फ़िल्मकारों, गीतकारों और संगीतकारों की कई पीढ़ियों ने हमें प्रेम सिखाने के लिए अपनी अनगिनत कल्पनाओं को फूँक दिया। किसी को पहली बार देखने के फ़न से लेकर, उससे टकरा जाने का हुनर तक हमें फ़िल्मों ने दिया है। इस प्रक्रिया में फ़िल्मों ने हमें लफंगा भी बनाया और अच्छा प्रेमी भी।
एक दूजे के लिए (1981) एक पावरफुल फ़िल्म थी। पहली बार हिन्दी सिनेमा में भाषा की दीवार लाँघकर प्रेमी उस महान भारत की कल्पना को साकार करने में अपनी जान देते हैं, जिसका ढोंग भारत दिन-रात करता है और ढिंढोरा भी पीटता है। रति अग्निहोत्री और कमल हसन की वो जोड़ी आज भी रुलाती है। इस फ़िल्म ने पहली बार हमारे भीतर की तथाकथित अखिल भारतीयता को चुनौती दी थी। ‘मेरे जीवन साथी/प्यार किए जा…’ — हिन्दी फ़िल्मों के नाम से गाने बना देना सिर्फ़ हुनर नहीं था, बल्कि एक रास्ता था कि अगर कोई हिन्दी वाली किसी तमिल वाले को चाहे तो मुमकिन है। वह उसके लिए हिन्दी फ़िल्मों के नाम से प्रेम की एक ज़बान गढ़ सकता है। और वो उसे चाहते हुए तमिलनाडु के ज़िलों और शहरों के नाम से बुला सकती है, बात कर सकती है और उसके साथ गा सकती है।
लेकिन फ़िल्मों ने हमें बहुत अच्छा प्रेमी नहीं बनाया। मुम्बई से आने वाली तमाम प्रेम कहानियाँ बहुत-से-बहुत अमीरी-ग़रीबी की दीवार से ही टकराती रह गईं। ‘चाँदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया/इक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया’ (विश्वास, 1969)। उफ़! अमीर लड़कियाँ हमेशा बेवफ़ा और दिल तोड़ने वाली होती हैं। वैसे कई फ़िल्मों में अमीर लड़कियों ने ग़रीब लड़कों के लिए घर-बार छोड़ा भी, लेकिन फ़िल्मों से यही नैरेटिव बना कि अमीरी-ग़रीबी इश्क़ की दुनिया की जात है, जिसके बीच प्रेम नहीं हो सकता। सब अपनी-अपनी जाति की हदों में रहें और हो सके तो वहीं प्यार की सम्भावना तलाशें।
हिन्दी सिनेमा के पर्दे पर अनगिनत प्रेमी जोड़े आए। पर्दे पर वो सिर्फ़ दो ख़ूबसूरत शरीर होते हैं। उनकी न तो कोई जाति होती है और न धर्म। हमारे फ़िल्मकारों की कल्पनाओं का प्यार वाक़ई कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं था। कभी गीतकारों ने अपनी क़लम से ऐसे गीत नहीं लिखे, जिनमें कोई लड़का किसी लड़की की सामाजिक पहचान से भिड़ जाता हो। सारे हीरो अपर कास्ट वाले हुए। कपूर, माथुर और सक्सेना से आगे नहीं जा सके। नायिकाएँ लिली, मिली और सिली होती रहीं। ऐसा लगा कि नायिका सीधे आसमान से आती है। ‘किसी शायर की ग़ज़ल, ड्रीम गर्ल/किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल’ (ड्रीम गर्ल, 1977) । ज़ाहिर है, हिन्दी सिनेमा की अनगिनत कहानियों ने इश्क़ को हैसियत के सवाल से जोड़ दिया, जबकि इश्क़ में आप स्टेटस-कोइस्ट हो ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको जाति की दीवार लाँघनी पड़ती है। हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रवचन देने वाली हिन्दी फ़िल्मों ने जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम इश्क़ को नज़रअंदाज़ किया। मुझे याद नहीं, कब किस फ़िल्म में कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के का हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किसी दलित लड़की के लिए कोई हीरो अपने कपूर खानदान को लात नहीं मारता। ओह, मैं भी फ़िल्मों से समाज-सुधार की उम्मीद करने लगा! कम ऑन, रवीश।
दरअसल जाति और मज़हब की दीवार तोड़कर प्रेम करने की कल्पना हमारी राजनीति में भी नहीं है। कुछ नेता हैं जो मुस्लिम हैं, मगर उनकी पत्नी हिंदू हैं। कुछ हिंदू नेता हैं, जिनकी पत्नी मुस्लिम हैं। बाक़ायदा प्रेम विवाह किया, मगर वे भी अपने इश्क़ को पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करते। बचते हैं कि कहीं मतदाता नाराज़ न हो जाए। लेकिन क्या समाज भी ऐसा है? बिलकुल है, मगर उसी के भीतर इश्क़ की ज़्यादा क्रांतिकारी सम्भावनाएँ पैदा होती रहती हैं। लोग जाति और धर्म की दीवार तोड़ देते हैं।
आपने ध्यान दिया कि मैंने कितनी बार ‘दीवार’ शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल, यही ट्रेजेडी है। इश्क़ बिना दीवार के कर नहीं सकते। बिना महबूब/महबूबा के कर सकते हैं, लेकिन बिना दीवार के नहीं! तमाम तरह के झमेलों से गुज़रना होता है प्यार में। आप पुरुष हों या स्त्री, बाग़ी और बावले हो जाते हैं। इतना टेंशन कि हिन्दी फ़िल्मों की तरह जल्दी किसी कल्पना में डिजॉल्व हो जाने का जी चाहता है, जहाँ अचानक पतलून और जूता सफ़ेद हो जाता है। महबूबा लम्बी सफ़ेद गाउन में स्लो मोशन में लहराती चली आती है। दोनों गाना गाने से पहले लिपट जाते हैं। ‘मय से मीना से न साक़ी से… ना पैमाने से/दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से’ (ख़ुदग़र्ज़, 1987) फ़िल्म के इस गाने से पता चला कि माशूका मनोरंजन का रिप्लेसमेंट हो सकती है। टीवी पर अच्छा गाना नहीं आ रहा हो, पिता से झगड़ा हो गया हो तो सारे टेंशन स्थगित कर कोई गाना गाया जाए। गुलज़ार या आनंद बख़्शी से लिखवाया जाए। Escape is the only space for love in India भारत में प्यार के लिए पलायन ही एकमात्र स्पेस है।
हमारे शहरों में प्रेम की कोई जगह नहीं है। पार्क का मतलब हमने इतना ही जाना कि गेंदे और बोगनवेलिया के फूल खिलेंगे। कुछ रिटायर्ड लोग दौड़ते मिलेंगे। दो-चार प्रेमी होंगे, जिन्हें लोग घूर रहे होंगे। कहीं बैठने की कोई मुकम्मल जगह नहीं है। इश्क़ के लिए जगह भी चाहिए। इस स्पेस के बिना हमारे शहर के प्रेमी सुपर मॉल के खम्भों के पीछे घंटों खड़े थक जाते हैं। कार की विंडो स्क्रीन पर पर्दा लगाए अपराधी की तरह दुस्साहस करते रहते हैं। सिनेमा हॉल के डार्क सीन में एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उजाले का सीन आते ही हाथ छोड़ देते हैं। प्रेम करने वालों ने अपनी ये व्यथा किसी को सुनायी नहीं। फ़ेसबुक पर भी नहीं लिखा। ‘मिलो न तुम तो हम घबराएँ, मिलो तो आँख चुराएँ, हमें क्या हो गया है’ (हीर राँझा, 1970) इस गाने को सुनते हुए क्या आपको नहीं लगता कि वह पूछे—पहले ये तो बताओ कि कहाँ मिलें?
लेकिन, हैट्स ऑफ़ टू ऑल लवर्स ऑफ़ इंडिया। मिलने की जगह नहीं, फिर भी आप मिलने की गुंजाइश ढूँढ लेते हैं। ऑटो का पर्दा गिरा देते हैं। पूरी पॉकेट मनी ऑटो के किराए में लुटा देते हैं। ख़ाली हॉल के चक्कर में बेकार फ़िल्मों का कलेक्शन बढ़ा आते हैं। आते-जाते लोगों की निगाहों के निशाने में रहने के बावजूद एक-दूसरे के कंधे से सिर नहीं हटाते। प्रेम के दो पल के लिए रोज़ हज़ार पलों की यह लड़ाई आपको प्रेमी से ज़्यादा एक्टिविस्ट बना देती है। जिसने भी प्यार किया है वह कम या ज़्यादा इन हादसों से गुज़रा ही है। मैं नेता होता तो हर शहर में एक ‘लव पार्क’ बना देता और अगला चुनाव ख़ुशी-ख़ुशी हार जाता। ज़ाहिर है, समाज को मेरी यह बात पसंद नहीं आती।
‘इश्क़ कोई रोग नहीं’ टाइप के सिंड्रोम से निकलिए। इश्क़ के लिए स्पेस कहाँ है, डिमांड कीजिए। पैंतीस साल के साठ प्रतिशत नौजवानो, तुम सिर्फ़ मशीनों के कल-पुर्ज़े बनाने और दुकान खोलने नहीं आए हो। तुम्हारी जवानी तुमसे पूछेगी, बताओ, कितना इश्क़ किया, कितना काम किया? काम से ही इश्क़ किया तो फिर जीवन क्या जिया? किसी की आँखों में देर तक देखते रहने का जुनून ही नहीं हुआ तो आपने देखा ही क्या? दहेज के सामान के साथ तौलकर महबूबा नहीं आती है। दहेज की इकोनॉमी पर सोसाइटी अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती, इसलिए वह लव मैरेज को आसानी से स्पेस नहीं देती। लड़की पहली कमोडिटी है जो लड़के के वैल्यू से तय होती है। पैसे के साथ दुल्हन! जबकि दुल्हन ही दहेज है! डूब मरो मेरे देश के युवाओ!
इश्क़ हमें इंसान बनाता है। ज़िम्मेदार बनाता है और पहले से थोड़ा-थोड़ा अच्छा बनाता है। सारे प्रेमी आदर्श नहीं होते और अच्छे भी नहीं होते, मगर जो प्रेम में होता है वह एक बेहतर दुनिया की कल्पना ज़रूर करता है। इश्क़ में होना आपको शहर के अलग-अलग कोनों में ले जाता है। आप किसी जगह हाथ पकड़कर चलते हैं तो किसी जगह साथ-साथ, मगर दूर-दूर चलते हैं! प्रेमी शहर को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उनकी यादों का शहर ग़ालिब की शायरी से अलग होता है। वो शहर को जानते भी हैं और जीते भी हैं। उन्हीं के भीतर धड़कती है मौसम की आहट। जो प्रेम में नहीं है, वह अपने शहर में नहीं है।
‘जिस तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊँ/जिस मन को लागे नयना, वो किसको दिखाऊँ’ (रुदाली, 1993)। आह! हम इश्क़ के अहसास को ज़ाहिर भी नहीं कर सकते । मीरा, तुम तो इसी देश की हो न!
इश्क़ हमें थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा संकोची बनाता है। एक बेहतर इंसान में ये कमज़ोरियाँ न हों तो वह शैतान बन जाता है। चाहना सिर्फ़ ‘आई लव यू’ बोलना नहीं है। चाहना किसी को जानना है और किसी के लिए ख़ुद अपने को भी जानना है। फ़रवरी का महीना है। किसी माशूक़ को ढूँढने में ही मत गँवा दीजिएगा। खोजिएगा ख़ुद को भी। अपने शहर को भी। उन कल्पनाओं को भी, जिन्हें आप किसी के लिए साकार करना चाहते थे।
हमें अपने शहर को इको-फ्रेंडली के साथ इश्क़-फ़्रेंडली बनाना है। एक स्पेस बनानी है, जहाँ हम सुकून के पल गुज़ार सकें। जहाँ किसी को देखते ही पुलिस की लाठी ठक-ठक न करे और किसी से बात शुरू करते ही बीच में बादाम वाला न आ जाए। ठीक है कि प्रेम के लिए स्पेस की कमी कल्पनाओं में नहीं है, फ़िल्मों में नहीं है। फिर शहरों में क्यों है? यह तो ठीक बात नहीं है।
पेरियार का लेख 'पति-पत्नी नहीं, बनें एक-दूसरे के साथी'