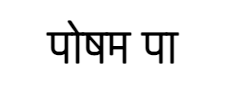निवेदिता मेनन की किताब ‘नारीवादी निगाह से’ में नारीवादी सिद्धातों की जटिल अवधारणाएँ और व्यावहारिक प्रयोग स्पष्ट और सहज भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। यह बतलाती है कि नारीवाद पूरे समाज के लिए ज़रूरी मसला है, यह सिर्फ़ महिलाओं का सरोकार नहीं है। यह निवेदिता की ख़ासी चर्चित पुस्तक ‘Seeing Like A Feminist’ का अनुवाद है, जो नारीवाद को पितृसत्ता पर अन्तिम विजय का जयघोष साबित करने के बजाय समाज के एक क्रमिक लेकिन निर्णायक रूपान्तरण पर ज़ोर देती है। नारीवादी निगाह से देखने का इसका आशय है मुख्यधारा तथा नारीवाद, दोनों की पेचीदगियों को लक्षित करना। इसमें जैविक शरीर की निर्मिति, जाति-आधारित राजनीति द्वारा मुख्यधारा के नारीवाद की आलोचना, समान नागरिक संहिता, यौनिकता और यौनेच्छा, घरेलू श्रम के नारीवादीकरण तथा पितृसत्ता की छाया में पुरुषत्व के निर्माण जैसे मुद्दों की पड़ताल की गई है। किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, प्रस्तुत है इसका किताब अंश—
परिवार क्या होता है? लोगों का एक समूह जो अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे के साथ खड़ा होता है? लेकिन अगर लोगों का कोई अन्य समूह ठीक यही व्यवहार करे तो उसे ‘परिवार’ के तौर पर मान्यता नहीं दी जाती। मसलन, दोस्तों की टोली, अविवाहित माँओं तथा अपने बहन-भाइयों के साथ रहनेवाली महिलाओं आदि को परिवार की संज्ञा नहीं दी जाती।
‘परिवार’ एक ऐसी संस्था है जिसके पास एक क़ानूनी पहचान होती है। और राज्य भी परिवार के उसी स्वरूप को मान्यता देता है जिसमें उसके सदस्य ख़ास तरह के सम्बन्धों में बँधे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क़ानून ही ‘परिवार’ की परिभाषा तय करता है; व्यक्ति को क़ानूनी दायरे के बाहर भी किसी न किसी परिवार का सदस्य होना पड़ता है और परिवार को हमेशा इसी संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत-सी हाउसिंग सोसायटियों में यह अलिखित क़ानून चलता है कि केवल विषमलिंगी विवाहित युगल को ही किरायेदार रखा जाएगा। इस तरह ‘परिवार’ केवल पितृसत्तात्मक, विषमलिंगी परिवार ही हो सकता है: एक पुरुष, एक स्त्री और पुरुष के बच्चे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 में अपने एक फ़ैसले में कहा था कि संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार परिवार पर लागू नहीं होते : ये अधिकार घर की ड्योढ़ी नहीं लाँघ सकते! न्यायाधीश का कहना था कि अगर मौलिक अधिकारों को परिवार के स्तर पर लागू कर दिया गया तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे ‘चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में साँड घुस आए।” यह न्यायाधीश बिलकुल सही फ़रमा रहे थे। अगर परिवार में मौलिक अधिकार लागू कर दिए जाएँ और परिवार के हरेक सदस्य को एक स्वतंत्र और समान नागरिक की तरह देखा जाने लगे तो परिवार नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी।
चूँकि अपने मौजूदा स्वरूप में परिवार जेंडर और उम्र की एक ऐसी दर्जाबन्दी पर टिका है जिसमें जेंडर अक्सर उम्र पर भारी पड़ जाता है। इसका मतलब है कि परिवार का वयस्क पुरुष किसी उम्रदराज़ महिला से ज्यादा ताक़तवर होता है।
इस तरह एक संस्था के रूप में परिवार ग़ैर-बराबरी पर आधारित है; इसका कार्य निजी सम्पत्ति के स्वामित्व के कुछ ख़ास रूपों तथा वंश अर्थात् सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार को पिता से शुरू करके पुत्रों तक ले जाना होता है। इसमें सम्पत्ति से और परिवार का ‘नाम’ पिता और पुत्रों तक सीमित रहता है।
मुझे हिन्दी फ़िल्म मृत्युदंड का एक दिलचस्प दृश्य याद आता है जिसमें माधुरी दीक्षित और शबाना आज़मी ने दो सगे भाइयों की पत्नियों की भूमिका निभायी है। शबाना का पति नपुंसक है और यह बात पूरा गाँव जानता है। कुछ समय के लिए वह अपने पति से दूर चली जाती है और किसी दूसरे आदमी से प्रेम करने लगती है; जब वह घर लौटकर आती है तो उसे देखकर सबको पता चल जाता है कि वह गर्भवती है। इस पर माधुरी दीक्षित बहुत हैरत से पूछती है कि दीदी, ये बच्चा किसका है? एक तरह से देखें तो यह सवाल ही बेतुका और ग़ैर-ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चा उसके शरीर के अन्दर है तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा उसी का होगा। लेकिन एक पितृसत्तात्मक समाज (केवल पितृसत्तात्मक समाज में ही) में यह बेतुका सवाल कि—बच्चे का बाप कौन है, पूरी तरह जायज़ माना जाता है। इस बच्चे की जाति क्या है? वह किसकी सम्पत्ति का वारिस बनेगा? इस पर शबाना छोटा-सा जवाब देती है : ‘मेरा’। मुझे याद है कि यह सुनते ही पूरे थिएटर में अजीब-सी चुप्पी छा गई थी। कुछ दबी-ढँकी खिलखिलाहट। और कुछ बेचैनी?
सच्चाई यह है कि पुरुष को इसका पता ही नहीं चल सकता कि बच्चा उसी का है या किसी और का। औरत को हमेशा पता होता है कि बच्चा उसी का है, लेकिन पुरुष डीएनए टेस्ट के बावजूद यह दावा नहीं कर सकता कि बच्चा उसी का है। डीएनए टेस्ट से केवल इतना पता चल सकता है कि बच्चा आपका है या नहीं; लेकिन अगर पुरुष के डीएनए का बच्चे के डीएनए से मिलान हो जाता है तो इससे केवल ‘सांख्यकीय दृष्टि से उच्च प्रायिकता’ का यह संकेत मिलता है कि अमुक बच्चा आपका है।
जैसा कि कहा जाता है, ‘मातृत्व एक जीव-वैज्ञानिक तथ्य है, जबकि पितृत्व केवल एक समाजशास्त्रीय कल्पना है।’
पितृसत्ता के लिए यह चीज़ एक स्थायी चिन्ता की बात होती है। यही चिन्ता स्त्रियों की यौनिकता पर पहरेदारी बिठाने की मानसिकता तैयार करती है।
वैलेंटाइन डे को लेकर जिस तरह का वितंडा खड़ा किया जाता है, वह दरअसल इस मुक्त ‘प्रेम’ के कथित तौर पर अन्तर्निहित ख़तरों की बानगी पेश करता है। भारत में वैलेंटाइन डे की लोकप्रियता नवें दशक के बाद लगातार बढ़ी है। नारीवादी वैलेंटाइन डे के ख़ास मुरीद नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें ‘रोमांस’ का यह आख्यान बहुत नहीं जँचता जिसमें प्रेम की एक ख़ास क़िस्म की कहानी को ही प्रेम की सच्ची कहानी माना जाता है। प्रेम की इस कहानी का ख़ास पहलू यह है कि उसे अनिवार्य रूप से स्त्री-पुरुष की कहानी होना चाहिए; और इसमें यह बात भी पहले से तय है कि जब कोई ‘प्यार में पड़ता’ है तो ज़्यादा सम्भावना इस बात की होती है कि वह ‘प्यार के लिए’ उचित व्यक्ति का चुनाव करता है। इस तरह, पुरुष की उम्र स्त्री से दो-चार महीने ज़्यादा होनी चाहिए; उसे स्त्री की तुलना में कम-से-कम दो इंच लम्बा होना चाहिए तथा उसकी कमाई स्त्री से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए! रोमांस के इस स्वरूप का कुल क़िस्सा ये है कि इसमें स्त्री हमेशा छोटी और प्यारी होनी चाहिए, जबकि पुरुष को पूरी तरह वयस्क दिखना चाहिए। इसलिए, हम नारीवादियों को ‘रोमांस’ के इस रूप से हमेशा परहेज़ रहा है जो दीवानावार होने के बजाय पितृसत्ता की गोदी में बैठना ज़्यादा पसन्द करता है।
हमें वैलेंटाइन डे से यह भी दिक़्क़त है कि वह ‘प्यार’ का कम, ख़रीद-फ़रोख़्त और बाज़ार का खेल ज़्यादा बन गया है क्योंकि इस दिन किसी को प्यार करना ही काफ़ी नहीं माना जाता। लोगों को अपना प्यार कार्ड, फूल और टैडी बेयर ख़रीदकर साबित करना पड़ता है। वैलेंटाइन डे की परिघटना नवें दशक की उपज है। यह वह दौर था जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी जा रही थी। उस समय हम इसकी आलोचना इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें यह नव-उपभोक्तावाद का सबसे सटीक उदाहरण लगता था।
लेकिन जल्दी ही यह हिन्दू दक्षिणपंथियों के निशाने पर आ गया और उसे ‘भारतीय मूल्यों’ के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यह घोषणा सिर्फ़ शाब्दिक नहीं थी; प्रेमी युगलों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार और मार-पीट की जाने लगी। वैलेंटाइन डे पर होनेवाले इन हमलों के साथ बड़े शहरों सहित पूरे देश में अपनी जाति या धार्मिक समुदाय से बाहर विवाह करनेवाले लोगों को जान से भी मारा जाने लगा। अंग्रेज़ी भाषी मीडिया में ऐसी हत्याओं को ‘ऑनर किलिंग’ कहा जाता है, लेकिन प्रतीक्षा बख्शी ने इसके लिए एक ज़्यादा स्याह और मुनासिब शब्द सुझाया है। प्रतीक्षा बख्शी ऐसी हत्याओं को ‘कस्टोडियल डैथ’ (हिरासत में होनेवाली मौत) की श्रेणी में रखना चाहती हैं क्योंकि ऐसे मामलों में तमाम युवा प्रेमियों, जिन्हें ख़ुद उनके परिवार ही बंधक बना लेते हैं, की मौत हिरासत के दौरान होती है। यही सूत्र हमें ‘समलैंगिक आत्महत्याओं’ में भी दिखायी दिया। हमारे सामने कई ऐसे मामले आए जिनमें आत्महत्या करनेवाली स्त्रियाँ अपने पीछे ख़त छोड़कर गई थीं जिनसे पता चला कि कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री से प्रेम करती थी; कि वह उसके बिना ज़िन्दा नहीं रह सकती थी लेकिन परिवार के लोग उन्हें एक-दूसरे से अलग करने पर आमादा थे। सार्वजनिक जीवन का ध्यान अपनी तरफ़ खींचनेवाली हिंसा की ऐसी हरेक घटना यह साबित करती है कि यौन शुचिता की जाति और समुदायगत कसौटियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
भीमराव आम्बेडकर समझ चुके थे कि ‘जाति के उन्मूलन’ में अन्तरजातीय विवाह एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 1936 में पहली बार प्रकाशित एक प्रसिद्ध लेख में उन्होंने कहा था : ‘जो समाज अन्य कड़ियों के कारण पहले से ही सुगठित होता है उसमें विवाह जीवन की एक सामान्य घटना होती है। लेकिन खण्डित समाज में विवाह एक संयोजक शक्ति की भूमिका निभाता है इसलिए वह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। जाति को तोड़ने के लिए अन्तरजातीय विवाह से ज़्यादा कोई उपाय कारगर नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी चीज़ जाति का ख़ात्मा नहीं कर सकती।’ (आम्बेडकर 1936 : 67)
ज़ाहिर है कि आम्बेडकर ने जिस अन्तरजातीय विवाह को जातिगत पहचानों का संहारक बताया था वह पिचहत्तर सालों बाद भी खाप पंचायतों के लिए भय का कारण बना हुआ है। परन्तु, नारीवादी होने के नाते हम विवाह को समाज की ख़ुशहाली के लिए स्वस्थ और संयोजक शक्ति मानने से इनकार करते हैं। इस मान्यता का औचित्य हम आगे स्पष्ट करेंगे।
आज इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में ‘ऑनर किलिंग्स’ नाम की इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल हरियाणा के जाट समुदाय की बहु-गोत्रीय ग्राम सभाओं-खाप पंचायतों के सन्दर्भ में बहुत होने लगा है। इस दौरान खाप पंचायतें ‘अनुचित’ विवाह करने की जुर्रत करनेवाले अनेक प्रेमी-युगलों को मौत का फ़रमान सुना चुकी हैं। इस प्रकार की पंचायतें ख़ुद को राज्य द्वारा स्थापित सरकारी पंचायतों से अलग रखकर देखती हैं और यह दावा भी करती हैं कि उनका जाति-समुदाय उन्हें सरकारी पंचायतों से ज़्यादा महत्त्व देता है। एक हद तक, यह बात सच भी मानी जा सकती है। खाप पंचायतें हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने की माँग भी करती रही हैं। उनकी माँग है कि अधिनियम के तहत सगोत्रीय तथा भाईचारे (पड़ोसी गाँवों के समूह) के क्षेत्र में होनेवाले विवाहों पर रोक लगनी चाहिए। अन्तर-जातीय विवाह के सामने पहले ही सामाजिक दबावों की दीवार खड़ी रहती है। ऐसे में, संयुक्त प्रतिबन्धों के कारण जवान होते किशोर-किशोरियों को अपने नज़दीकी दायरे में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे वे प्रेम कर सकें। इसका मतलब है कि एक ही जाति के युवा बहुत नज़दीकी माने जाएँगे जबकि असम्बन्धित लोगों को दूसरी जाति का घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह विवाह से जुड़े तमाम फ़ैसले परिवार के हाथों में सिमट जाएँगे।
इस सम्बन्ध में अक्सर कहा जाता है कि खाप पंचायतों की हिंसक और स्वेच्छाचारी छवि के पीछे शहरी और अंग्रेज़ीदाँ इलीट का हाथ है जो देहाती लोगों के प्रति विकट तिरस्कार का भाव रखते हैं, जबकि सम्बन्धित समुदाय को खाप पंचायतों के क्रिया-कलापों से कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन, यहाँ यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि खाप पंचायतों की सत्ता को पहली चुनौती इन्हीं समुदायों के युवाओं से मिलती है। सच तो ये है कि ‘शहरी इलीट’ के सामने यह मुद्दा आया ही इसलिए क्योंकि इन समुदायों के युवा लड़के-लड़कियाँ खाप पंचायतों के फ़रमानों का पूरी ताक़त से प्रतिरोध करते हैं और अपने प्रेम के लिए सामाजिक बहिष्कार; यहाँ तक कि मौत क़ुबूल करने के लिए भी तैयार रहते हैं। (यह इतना विषादपूर्ण है कि यहाँ मैं प्रेम और रोमांस के विषय में अपनी परम्परा-भंजक समझ को एक क्षण के लिए विराम देना चाहती हूँ!)
संक्षेप में, भारतीय समाज की पुरातनपंथी ताक़तों की तरह नारीवादी भी वैलेंटाइन डे के ख़तरे को समझते हैं। वे जानते हैं कि प्रेम बने-बनाए ढाँचे को उलटकर रख देता है और जाति, समुदाय तथा विषमलिंगी यौनिकता के नियमों में बँधने से इनकार कर देता है।
कृष्णा सोबती के उपन्यास 'मित्रो मरजानी' से एक अंश