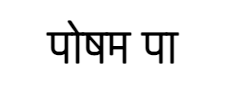1
इश्क़,
तुम मेरी ज़िन्दगी में आओ तो यूँ आओ
कि जैसे किसी पिछड़े हुए गाँव में
कोई लड़की घण्टों रसोई में खपने के बाद
पसीने से भीगी बाहर आए
और ठीक उसी वक़्त बिजली आ आए।
2
हमें लोहा चाहिए था—
हथियार बनाने को नहीं,
ख़ून में घुल जाने को।
अफ़सोस कि
हमारे ख़ून से जन्म लेने वालों ने
सब हथियार हम पर ही आज़माए।
3
चाची घर-भर के लिए रोटियाँ सेंकती है—नर्म-मुलायम
और कोई रोटी अगर जल जाए तो चाची ही के हिस्से आती है।
चाची की पक्की रसोई में और एक रोटी सेंकने भर गुँथा आटा है
चाची के अहाते की घड़ी में और एक रोटी सेंकने लायक़ वक़्त है
चाची के मज़बूत हाथों में और एक रोटी सेंकने की सकत है
चाची के पास एक रोटी जला देने भर के अपराध-बोध से
मुक्त हो जाने की सुविधा नहीं है,
इस अपराध-बोध को रोटी समझ गले उतारने
या चारा समझ भैंस के सामने डालने की दुविधा है
बहुत लफ़्फ़ाज़ी जान पड़ती है न यह सब?
सच है मगर
हर टोले-गाँव-पिण्ड-जवार होती हैं ऐसी चाचियाँ
कि जिनके लिए बाइस दिवस चुभने वाली शूल है
वो
जो
तुम्हारे-मेरे लिए
अल्हड़-सी भूल है।
4
एक रहस्यमय श्रमिक
कड़ी धूप में बिना थके
चलाता रहता था हथौड़ा
तोड़ना चाहता था पहाड़
मस्तक पर स्वेद की बूँदें
नेत्रों में थी विश्वास की ज्वाला
लोग आश्चर्य करते
कौन है वो
कहाँ से प्राप्त होती है
अनवरत परिश्रम की शक्ति उसे
चैत्र की एक साँझ जाने कैसे
हथौड़ा उसके पाँव पर पड़ गया
लोगों ने देखा
उसके घाव से रक्त नहीं
पिघला हुआ लोहा बह रहा था
सबके हृदय में प्रश्न थे
सब जानना चाहते थे
उसका परिचय
श्रमिक ने अपने घाव से दृष्टि हटायी
एक लम्बी साँस ली और कहा—
“मेरी माँ थी वो स्त्री
देखा था जिसे ‘निराला’ ने
तोड़ते हुए पत्थर
इलाहाबाद के पथ पर!!”
5
उन्हें मोह नहीं किसी से
क्या सगा, क्या पराया
सबकी देह में निरपेक्ष भाव से उतारते हैं विष
उनके स्पर्श तक को लोग मृत्यु कहते हैं
वे कहीं ठहरकर नहीं रहते
घर को घर नहीं कहते
वे भागते हैं बहुत बार जागते हुओं से
और बहुत बार सोते हुओं की कभी न टूटने वाली नींद के दोषी होकर भी
नहीं रखते अपराध-बोध कोई, न ही कोई दण्ड सहते हैं
यूँ तो सर्पों के विषय में कही गई बातें हैं ये
पर अचम्भा तो देखो
सच है उन मनुजों के लिए भी
जो होते हैं सबके मित्र, शत्रु किसी के नहीं
और डसते उन्हें हैं जिनकी आस्तीनों में रहते हैं!
6
मेरी अलिखित
कविता की
मरी हुई नायिका
मुझसे मेरे हिस्से की
दो मुट्ठी मिट्टी माँगती है
और मैं, बदले में
उसकी क़ब्र में
सो जाने की
कामना करती हूँ
मुझे मेरे तुच्छतम बलिदानों का श्रेष्ठतम प्रतिफल।
7
मेरे शब्दकोश में
अन्तिम का अर्थ आँसू था
अन्तिम भेंट, अन्तिम प्रेम… अन्तिम इच्छा
हर अन्तिम ने अन्ततः आँसुओं की भेंट चढ़ना चुना
सन्तोष रहता मुझे जो तुम जीवन में बने रहते
यूँ जीवन के अन्तिम दुःख का अर्थ आँसू नहीं रह जाता!
8
रात मुझे सुलाने को व्यूह सजाती है
रात को मैं काट खाने दौड़ती हूँ
मैं चिड़िया के से दिल वाली ऐसी कठोर कब थी
कि ख़ुश्क पत्थर-आँखें पलकों की झपकन पर पाबन्दी लगा देतीं
या कि पलकों नींद उकेरने की बातें माथे नागफनियाँ उगा देतीं
क्यों न हुआ यह
कि नींद आँखों की तरलता में खाद-पानी तलाशती
सपने उसी नींद में डूब-डूब उबरते
क्योंकर हुआ यह
कि सपनों से भागी मैं बावली हुई फिरती हूँ
नींद मेरे सिर से टकराकर अपने टुकड़े सहेजती है।
9
प्रकाश भ्रमित करता है मुझे
जैसे भ्रमर को भ्रम में रखते हैं पुष्प
जैसे भयाक्रान्त रहती है मित्रता छल से
वैसे ही ठीक, दीप्ति से मुझे भय आता है
जब निद्रा-मग्न हो संसार समग्र
तो भींच लेता है स्वयं में
मुझे मुझसे मिलाता है, बूझो कौन?
‘अंधकार’
जो आश्रय है मेरा
मुझे जाग का पाठ पढ़ाता है
इसी पाठ का प्रताप है
कि
मैं रात्रि-उदिता
दिवाकर से मानती हूँ
बैर जाने कौन जनम का
यूँ कि जो भूले से भी पड़ूँ दिवस के फेर में
तो मूँद रखती हूँ नेत्र अपने
‘तमस-तमस’ उच्चारती हूँ
सशंकित हूँ शशि से भी
सो करती हूँ त्याग सुख-चंद्रिका का
अमावस का नैकट्य स्वीकारती हूँ।
10
वह ध्वनियों का आखेटक था
और उस बसन्त मेरे गले में शूल अटकते थे
चिड़ियों का चहचहाना सपने में सुन उठ बैठने वाला वह
हवा की सरसराहट पर जाने क्या सुन मुस्कुराने वाला वह
अब कुछ सुनना नहीं चाहता था
मैं उसे सुनायी पड़ने की सब कोशिशें करती
बहुत शोर करने वाले जूते पहनती
सबसे ज़्यादा खनकने वाली चूड़ियों से कलाई दुखाती
और तो और, उसे सुनाने को सपनों में काँच चबाती
उस तक कुछ नहीं पहुँचता
मैं उसकी आँखों में गहरी खाई-सा ख़ालीपन देखती
जिसमें मरती हुई आवाज़ों की गूँज थी
मैं घबराकर अपने ही दिल पर हाथ रखती
कोई जवाब नहीं आता
उसके होंठों की बदलती मुद्राओं के बीच
मैं खिलखिलाहट सुनना चाहती
उसकी हँसी के जवाब में
अपनी हँसी उस तक पहुँचाना चाहती
पर जाने कैसे मेरे और उसके बीच निर्वात आ जाता
ये वे दिन थे
जब मैं ध्वनि से शब्दों को छानने की कोशिश में
ज़ुबान पर राख मलती थी
ये वे दिन थे
जब ध्वनियों का आखेटक मौन-देस में विचरता
ध्वनियों का स्वाद भूल गया था।
कविताएँ साभार: विक्रांत (शब्द अंतिम)
'स्त्रियों ने कोई कृत्रिम धर्म क्यों न बनाया?'