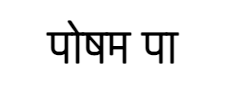सम्वाद महज़ शब्दों से तो नहीं होता। जब शब्द चूक जाते हैं, तब स्पर्श की अर्थवत्ता समझ आती है। ग़ालिब कहते हैं— “मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यूँ रात-भर नहीं आती”—यहाँ मिर्ज़ा की चिंता जायज़ है। उनका प्रश्न लाज़िम है। नींद का न आना मृत्यु के भय से आक्रांत होने का कारण है। आज के परिवेश में इस शे’र के दूसरे मिसरे के प्रश्न का उत्तर मौजूद है। एक होता है समय से जाना, एक होता है बे-समय जाना। कोई बे-समय जाना नहीं चाहता। किसी का बे-समय जाना आहत करता है। सत्ता की लापरवाही और बदइन्तज़ामी के कारण जिस तरह से ज़िंदा आदमी आँकड़ों में तब्दील हो रहा है, उसने यह साबित कर दिया है कि हमारी प्राथमिकताएँ ग़लत थीं। हमारा चुनाव ग़लत था।
मुझे याद है, मेरे दोस्त के पिताजी बीमार थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक-दो महीने उनका इलाज चला था। कई रातें मैंने वहाँ के परिसर में दोस्त के साथ काटी थीं। दुश्चिन्ताओं के बीच नींद नहीं आती थी। रात के बीतते पहर में जब नींद आती, सामूहिक विलाप नींद के किवाड़ को पीट-पीटकर जगा देता था। पता चलता था किसी परिवार ने किसी अपने को खो दिया। किसी अपने को खोना एक यात्रा का अंत ही तो है। जिसके साथ आपने एक उम्र जी हो, उसकी आवाज़, उसका सम्बोधन, उसका स्पर्श सब याद बनकर रह जाता है।
खोने का डर जब सपनों तक पहुँचता है, तब नींद नहीं टूटती, इंसान टूटता है।
शिवेंद्र का एक उपन्यास है ‘चंचला चोर’, उसमें वे एक जगह लिखते हैं— “हम कोशिकाओं से नहीं, स्मृतियों से बने हैं।” कितनी सच्ची और प्यारी बात है। विज्ञान देह को अच्छी तरह समझता है, लेकिन उसने मन को अभी भी बहुत कम जाना है। शिवेंद्र लोक कथाओं के मार्फ़त जो यथार्थ, जो विमर्श रचते हैं, वह काफ़ी सराहनीय है। कई बार उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगा कि जिस कहानी को बचपन के दिनों में मेरी नानी सुनाया करती थीं, उस कहानी की उत्तर कथा शिवेंद्र अपनी कल्पना से रचते हैं। इसी उपन्यास में एक जगह वे लिखते हैं— “डायरी अकेले छूट जाने की छटपटाहट है और लेखक होना प्यार न किए जाने का सबूत।” लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ? शायद इसलिए कि कहने को बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। दीवारें सुनकर जवाब भी तो नहीं देतीं। शायद इसलिए भी कि कुछ लिखकर ज़िंदा महसूस होता है। कल को मैं न रहूँ, मेरा लिखा तो रहेगा न।
* * *
हर चेहरा बीमार-सा दिखता है। यह समय भी। आने वाले समय में जो इस बीमारी से बचे रह जाएँगे, वे अगली पीढ़ी को इस समय का क़िस्सा सुनाएँगे। बहुत सम्भव है, क़िस्सा सुनाते-सुनाते वे चुप हो जाएँ। हाँ, इस भयावह समय को याद करना भी उतना ही मुश्किल होगा जितना मुश्किल इसे अभी जीना है। हम क्षणों में जीते हैं। हमें जीया हुआ सबकुछ याद नहीं रहता। हमारा दिमाग़ बहुत ही चतुराई से धीरे-धीरे वह सब मिटाते जाता है जो उपेक्षित है। हमें कुछ क्षण याद रहते हैं। न पूरा बचपन, न पूरी जवानी। लेकिन यह समय, यह बुरा समय बचे हुए लोगों के ज़ेहन में रहेगा।
हमारी यादों में यह समय उपेक्षित होते हुए भी संरक्षित रहेगा। हम जब भी याद करेंगे खोया हुआ कोई चेहरा, यह समय याद आएगा। हम जब भी चूमेंगे किसी का माथा, यह समय याद आएगा। हम जब भी किसी को बाहों में भरेंगे, यह समय याद आएगा।
कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देखी। एक पत्नी कोरोना से संक्रमित अपने पति के आख़िरी क्षणों में उसे अपने मुँह से साँस देने की बदहवास कोशिश कर रही थी। मृत्यु के सम्मुख मनुष्य कितना लाचार हो जाता है। हम अपने प्रिय को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। एक दोस्त हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके अपने दोस्त के लिए ऑक्सीजन का सिलेण्डर लाता है। डॉक्टर्स, नर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सभी लोग अपने-अपने स्तरों पर जुटे हुए हैं। यही सब है जो क़िस्सा बनेगा। ज़िंदा रहेगा। प्रियम्वद अपने उपन्यास ‘वे वहाँ क़ैद हैं’ में दादू के हवाले से कहते हैं—
“काल के प्रवाह में सत्ताएँ नष्ट होती हैं। व्यक्ति नष्ट होते हैं। देश, नगर, सभ्यताएँ नष्ट होती हैं। यह तुम्हें इतिहास बताएगा पर यह तुम्हें ख़ुद ढूँढना होगा कि इन अंधेरों में जब सब नष्ट होता है, तब भी एक चीज़ अक्षत, अक्षुण्ण रहती है और वह है मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता, उसकी गरिमा पर आस्था और उस आस्था के कभी न क्षरित होने की आशा।”
इस भयावह समय में दुनिया-भर से आ रहीं मनुष्यता की ख़बरें, आस्था की तस्वीरें आशाओं और उम्मीदों का कोलाज रच रही हैं। जो इतिहास में दर्ज हो न हो, क़िस्सों में कहा जाएगा, क़िस्सों में सुना जाएगा। इसी से आदमी का विश्वास बना रहेगा। जो टूटने के बाद भी बचा रहे, वही सुन्दर है।
* * *
कभी-कभी दिन छोटा और रातें लम्बी होती हैं। इन दिनों दिन भी लम्बा और रातें भी लम्बी लग रही हैं। इतना सन्नाटा है चारों तरफ़ कि छत से झूलते पंखे की आवाज़ कानों को चुभती है। उसकी गति कम करता हूँ तो गर्मी लगती है और तेज़ करता हूँ बेचैनी होती है। कुछ भी सामान्य नहीं है।
यह दौर ही असामान्य है जिसमें आदमी लगातार सामान्य होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सामान्य होने की कोशिश करना भी तो असामान्य होने का लक्षण है।
कभी-कभी लगता है दरवाज़ा खुल रहा है लेकिन अचानक से मुँह पर आकर फटाक से बंद हो जाता है। एक आदमी कितनी ख़्वाहिशें लेकर शहर आता है। कितना कुछ छोड़ आता है अपने पीछे; अपने लोग, अपना शहर, अपना गाँव, अपना घर। हम कितनी कोशिश करते हैं, नए शहर में ख़ुद को ढालने की। नए शहर से मिलते-जुलते एक लम्बा समय बीत जाता है। नया शहर हमें पहचानने लगता है और अपना शहर हमें भूलने लगता है। हम भी अपने शहर को भूलने लगते हैं। एक आदमी कितनी संज्ञाओं के साथ जन्म लेता है, बड़ा होता है और मर जाता है। जब संकट का समय आता है, जब लगता है दूर-दूर तक कोई नहीं है, जब लगता है अंधेरा और गहरा होने वाला है, ऐसे समय में सबसे पहला हमला सभी संज्ञाओं पर ही होता है।
बहुत-सी चीज़ें हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। परिभाषाओं की परिधि में सबकुछ नहीं आ सकता। परिधि के बाहर जो कुछ छूट जाता है, धीरे-धीरे वह हमारे ख़याल से भी बाहर चला जाता है। हम उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। हमें तमाम परिभाषाओं के विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी होगी। इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं।
* * *
मृत्यु महज़ देह का अंत नहीं है। यह पूर्णविराम है एक सफ़र का। यहाँ से आप चाहकर भी उस इंसान के साथ आगे की यात्रा तय नहीं कर सकते जो अब इस संसार में नहीं है। एक यात्रा स्मृतियों की होती है जहाँ हम बीता हुआ कुछ पा लेते हैं। लेकिन हम वहाँ ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का पैर सामने की ओर होता है। क्या होता अगर हम पीछे की ओर भी उसी तेज़ी से भाग सकते जितनी तेज़ी से सामने की दिशा में भागते हैं?
आज मेरे चचेरे दादा जी का देहांत हो गया। इसी साल जनवरी में घर गया था तब मुलाक़ात हुई थी। आख़िरी मुलाक़ात। सोकर उठते ही मोबाइल देखने पर यह ख़बर मिली। कल तक सबकुछ ठीक था। वे चल-फिर रहे थे। स्मृतियों का भार सीने पर महसूस कर रहा हूँ। महामारी और इसका भय गाँव में भी फैल चुका है। महामारी के डर से गाँव के लोग दूर से ही देखते रहे। अमूमन गाँव में ऐसा होता नहीं है। आज आदमी को आदमी से ख़तरा है। हम किस बुरे दौर से गुज़र रहे हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज एक परिचित पार्थिव शरीर भी भय का कारण है। यह कैसा अंत है? कितना भयानक अंत है!
पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें याद कर रहा हूँ तो बार-बार फाइलेरिया से ग्रसित उनका फूला हुआ पैर स्मृति में कौंध जा रहा है। यह अस्थायी पहचान न जाने कब उनकी देह में स्थायी रूप से चिपक गई थी, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं। आजकल ख़बरें चौंका रही हैं। प्रायः घर से एक नियत समय पर ही कॉल आता है। इन दिनों अनियत समय पर घर से आया कॉल आकस्मिक भय भी ला रहा है। फ़ोन रखते हुए दोनों तरफ़ से आख़िरी बात होती है—
“अपना ख़याल रखना।”
बिखरा-बिखरा, टूटा-टूटा : कुछ टुकड़े डायरी के (पहला भाग)