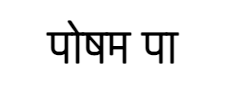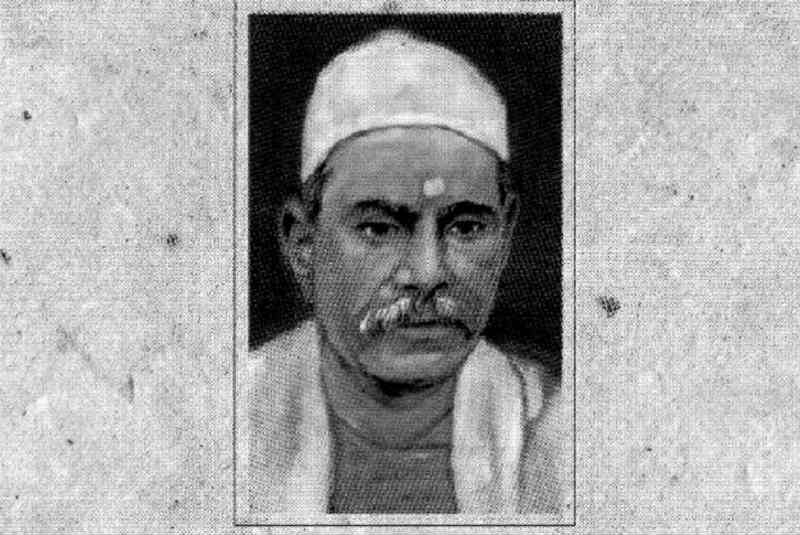इतिहासों से पता लगता है कि असभ्य से असभ्य जाति भी गुलामी के बंधन से छुट तरक्की और सभ्यता की चरम सीमा को पहुँच गई है। हमने अपने पहले के वैदिक ऋषियों के क्रम को छोड़ने के साथ ही दास्य भाव को ऐसा गहरे पकड़ रखा है कि उससे अपना छुटकारा करना चाहते ही नहीं – जहाँ का धर्म दास्य भाव लिखाता है उस जाति की गुलामी का भला क्या कहना?
कोई भक्त प्रगाढ़ भक्ति के उद्गार में भर अपने सेव्य प्रभु से कहता है-
“त्वद् भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्य भृत्यभृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ”
हे प्रभो लोकनाथ। आप अपने दास का दास का दास का दास समझ मुझे याद रखिए। नीचे ही ताक रहा है ऊपर को सिर उठाने का मन ही नहीं करता। इसमें संदेह नहीं ऐसे भक्त जनों का चित्त बड़ा ही विमल, कोमल, सरल और उदार रहा। उन्हें महात्मा और सत्पुरुष मान समाज उनके पीछे दौड़ी और उनका अनुसरण करने लगी। पर चित्त-वृत्ति उन भक्त जनों की कैसी कोमल, सरल और अकुटिल थी सो तो ले न सके, दास बनने की बाहरी बात अपने में आरोपित कर दासोस्मि दासोस्मि कहने लगे। कहने क्या लगे, जन्म-जन्म के दास और गुलाम दर गुलाम हो ही गए। तब इनके यावत् क्रम जितनी बात सब गुलामों की सी हो गई। जिनमें गुलामी की दुर्गंधि की दूर ही से ऐसी भभक उड़ती है कि सैकड़ों वर्ष तक सभ्यता के गुलाब और केवड़े का इत्र भी अपना असर वहाँ पहुँचा उसे सुगंधित नहीं कर सकता। न उस बदबू को दूर कर सकता है। काम तो हमारे दास्य भाव के ही है नाम से तो गुलाम न बनते.. सो हम लोगों में अधिकांश नाम रामदास भगवानदास ऐसे करीह और कटु लगते हैं कि सुनते ही घिन पैदा हो जाती है।
मनु ने शर्मा, वर्मा और गुप्त ये तीन उपाधियाँ द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए रखी है। शर्म माने सुख के हैं, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व के उज्जवल संस्कार अनुसार उज्ज्वल कर्म करता हुआ सबों को सुख पहुँचाता रहे। इसी तरह वर्मा के अर्थ रक्षा के हैं, क्षत्रिय अपने बल वीर्य से सबों की रक्षा करे। ऐसा ही गुप्त के अर्थ भी रक्षा या छिपाना है। वैश्य हर तरह बनिज व्यापार कर प्रजा का धन बचाता और बढ़ाता रहे। उसी के अनुसार नाम भी इन तीनों के ऐसे होने चाहिए जिनसे उन-उन अर्थों का बोध हो, न कि सब के सब दास बन बैठे। कहने मात्र को द्विज रहे वास्तव में काम और नाम दोनों से सब के सब शूद्र क्या बल्कि उससे भी बदतर हैं।
बुद्धिमानों ने उपाय और अपाय दो बात निश्चय किया है।
“उपायांश्चिन्तयेत्प्राज्ञस्
किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए उपाय करें और उपाय में कृत कार्य होने पर जो अपाय विघ्न दूसरी बात उठ खड़ी हो उसके हटाने की भी तदबीर सोच रखें। भक्ति मार्ग वालों ने चित्त को विमल और कोमल रखने की सुगम उपाय नवधा भक्ति बहुत अच्छा सोचा पर उसके साथ ही हमारी अज्ञानता कितना बढ़ेगी सो बिलकुल न सोचा। उसी अज्ञानता का परिणाम हमारे कौमी जोश पर जा टूटेगा इसका कहीं शानगुमान भी उन्हें न रहा। अस्तु जाय बहै कौमी जोश और देशानुराग चित्त का विमल और शुद्ध होना ही क्या कम बरकत है सो इस समय के कोरे मुर्ख कुंदे नातराश भक्तों में वह भी नहीं पाया जाता।
जड़ प्रतिमा में तो बड़ा ही भाव, भक्ति और प्रेम प्रकट करेंगे, पर सजीव अपने किसी दुखी भाई को देख पिघल उठना एक ओर रहा, निठुराई के साथ उसको हानि पहुँचाने से न चूकेंगे। क्या यही उनके भक्ति मार्ग का तत्व है? इस भक्ति ने जैसा दास्य भाव को पुष्ट कर रखा है वैस और ने नहीं। भक्ति के साथ वीररस मिला रहता तो कभी इससे हानि न पहुँचती किंतु भक्तिमार्ग का प्रादुर्भाव तब हुआ जब देश में सब और मुसलमानों की हुकूमत अच्छी तरह जम गई थी और आर्य जाति अपनी वीरता में च्युत हो चुकी थी। मुसलमानों का संपर्क पाय उनकी सी भोग-लिप्सा इनके मन में स्थान पा चुकी थी। परिणाम में भक्ति के साथ श्रृंगार रस मिल गया। श्रृंगार में सनी इसी भक्ति ने योगिराज हमारे कृष्ण भगवान को अत्यंत विलासी और रहस्य प्रिय बना दिया। नहीं तो कैसे संभव था कि जिन्होंने गीता का ज्ञान कहा था, जिनकी राजनैतिक काटव्योंत ने महाभारत का युद्ध कराया, बड़े-बडे़ महारथी वीर बांकुरे राजाओं को युद्ध में कटवाया, भारत-भूमि निर्वीर्य करवा डाला वह ऐसे भोग-विलासी होते।
श्रृंगार और वीर दोनों विरोधी रस हैं, एक ही ठौर दोनों नहीं ठहर सकते। महाभारत के युद्ध के उपरांत बुद्धदेव ने अहिंसा परमोधर्म का शिक्षा से दया विस्तार कर वीरता की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाया, पीछे भक्ति के साथ श्रृंगार रस मिला प्रजा को आशिकतम भोग लिप्सू कर डाला। बडे़-बडे़ राजा भी भक्त बन बैठे। महाभारत के समय का युद्धोत्साह और रण भूमि का प्यार न रहा तो बाहरी शत्रुओं से लड़ता कौन? परस्पर की स्पर्द्धा और फूट का अंकुर महाभारत ही के समय से जम चुका था.. जयचंद्र और पृथ्वीराज के समय वही फूट का बीज वृक्ष के रूप में परिणत हो फलों सें लद गया। उधर क्षत्रियों के बीच से वीरता डेरा डंडा उठाए बिदा हुई, इधर ब्राह्मण तप: स्वाध्याय संतोष संपत्ति का विसर्जन कर लालची बन वैदिक ऋषियों की आप्तता और ज्ञान खो बैठे। निर्बल और पौरुष विहीन हो जाने से जैसा ईश्वर का सहारा लेना सूझता है, वैसा तब नहीं जब हममें बल और सामर्थ्य मौजूद है। भक्ति और प्रतिभा से एक बड़ा लाभ अवश्य हुआ कि जब अत्याचारी मुसलमान देश भर को दीन इसलाम का पैरोकार किया चाहते थे और हमारे धर्म ग्रंथों को जला कर उच्छिन्न कर रहे थे, उस समय इसी भक्ति और प्रतिमा ने हिंदुआनी की जड़ कायम रखा। जड़ बनी रह गई तो अब इस समय सभी रिफार्मर बनते हैं और गाल फुलाए-फुलाय हमें सत्य धर्म सिखा रहे हैं।