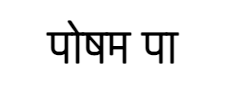मरने से एक दिन पहले तक उसे अपनी मौत का कोई पूर्वाभास नहीं था। हाँ, थोड़ी खीझ और थकान थी, पर फिर भी वह अपनी ज़मीन के टुकड़े को लेकर तरह-तरह की योजनाएँ बना रहा था, बल्कि उसे इस बात का संतोष भी था कि उसने अपनी मुश्किल का हल ढूँढ निकाला है और अब वह आराम से बैठकर अपनी योजनाएँ बना सकता है। वास्तव में वह पिछले ही दिन, शाम को, एक बड़ी चतुराई का काम कर आया था—अपने दिल की ललक, अपने जैसे ही एक वयोवृद्ध के दिल में उड़ेलने में सफल हो गया था। पर उसकी मौत को देखते हुए लगता है मानो वह कोई नाटक खेलता रहा हो, और उसे खेलते हुए ख़ुद भी चलता बना हो।
एक दिन पहले, जब उसे ज़मीन के मामले को लेकर, डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर में जाना था तो वह एक जगह, बस में से उतरकर पैदल ही उस दफ़्तर की ओर जाने लगा था। उस समय दिन का एक बजने को था, चिलचिलाती धूप थी, और लम्बी सड़क पर एक भी सायादार पेड़ नहीं था। पर एक बजे से पहले उसे दफ़्तर में पहुँचना था, क्योंकि कचहरियों के काम एक बजे तक ही होते हैं। इसके बाद अफ़सर लोग उठ जाते हैं, कारिंदे सिगरेट-बीड़ियाँ सुलगा लेते हैं और किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते, तब तुम कचहरी के आँगन में और बरामदों में मुँह बाए घूमते रहो, तुम्हें कोई पूछता नहीं। इसीलिए वह चिलचिलाती धूप में पाँव घसीटता, जल्दी से जल्दी डिप्टी-कमिश्नर के दफ़्तर में पहुँच जाना चाहता था।
बार-बार घड़ी देखने पर, यह जानते हुए भी कि बहुत कम समय बाक़ी रह गया है, वह जल्दी से कदम नहीं उठा पा रहा था। एक जगह, पीछे से किसी मोटरकार का भोंपू बजने पर, वह बड़ी मुश्किल से सड़क के एक ओर को हो पाया था। जवानी के दिन होते तो वह सरपट भागने लगता, थकान के बावजूद भागने लगता, अपना कोट उतारकर कंधे पर डाल लेता और भाग खड़ा होता। उन दिनों भाग खड़ा होने में ही एक उपलब्धि का-सा भास हुआ करता था—भागकर पहुँच तो गए, काम भले ही पूरा हो या न हो। पर अब तो वह बिना उत्साह के अपने पाँव घसीटता जा रहा था। प्यास के कारण मुँह सूख रहा था और मुँह का स्वाद कड़वा हो रहा था। धूप में चलते रहने के कारण, गर्दन पर पसीने की परत आ गई थी, जिसे रुमाल से पोंछ पाने की इच्छा उसमें नहीं रह गई थी।
“अगर पहुँचने पर कचहरी बंद मिली, डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार आज भी नहीं आया तो मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाऊँगा—किसी बेंच पर, दफ़्तर की सीढ़ियों पर या किसी चबूतरे पर—कुछ देर के लिए दम लूँगा और फिर लौट आऊँगा। अगर वह दफ़्तर में बैठा मिल गया तो मैं सीधा उसके पास जा पहुँचूँगा—अफ़सर लोग तो दफ़्तर के अंदर बैठे-बैठे गुर्राते हैं, जैसे अपनी माँद में बैठा कोई जंतु गुर्राता है—पर भले ही वह गुर्राता रहे, मैं चिक उठाकर सीधा अंदर चला जाऊँगा।”
उस स्थिति में भी उसे इस बात का भास नहीं हुआ कि उसकी ज़िन्दगी का आख़िरी दिन आ पहुँचा है। चिलचिलाती धूप में चलते हुए एक ही बात उसके मन में बार-बार उठ रही थी—काम हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस, काम हो जाए।
उससे एक दिन पहले, तहसीलदार की कचहरी में तीन-तीन कारिंदों को रिश्वत देने के बावजूद उसका काम नहीं हो पाया था। कभी किसी चपरासी की ठुड्डी पर हाथ रखकर उसकी मिन्नत-समागत करता रहा था, तो कभी किसी क्लर्क-कारिंदे को सिगरेट पेश करके! जब धूप ढलने को आयी थी, कचहरी के आँगन में वीरानी छाने लगी थी और वह तीनों कारिंदों की जेब में पैसे ठूँस चुका था, फिर भी उसका काम हो पाने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे तो वह दफ़्तर की सीढ़ियों पर आ बैठा था। वह थक गया था और उसके मुँह में कड़वाहट भरने लगी थी। उसने सिगरेट सुलगा ली थी, यह जानते हुए कि भूखे पेट, धुआँ सीधा उसके फेफड़ों में जाएगा। तभी सिगरेट के कश लेते हुए वह अपनी फूहड़ स्थिति के बारे में सोचने लगा था।
“अब तो भ्रष्टाचार पर से भी विश्वास उठने लगा है”, उसने मन-ही-मन कहा, “पहले इतना तो था कि किसी की मुट्ठी गर्म करो तो काम हो जाता था, अब तो उसकी भी उम्मीद नहीं रह गई है।”
और यह वाक्य बार-बार उसके मन में घूमता रहा था।
तभी उसे इस सारी दौड़-धूप की निरर्थकता का भास होने लगा था : यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 73 वर्ष का हो चला हूँ, अगर ज़मीन का टुकड़ा भी मिल गया, उसका स्वामित्व भी मेरे हक़ में बहाल कर दिया गया, तो भी वह मेरे किस काम का? ज़िन्दगी के कितने दिन मैं उसका उपभोग कर पाऊँगा? बीस साल पहले यह मुक़दमा शुरू हुआ था, तब मैं मनसूबे बाँध सकता था, भविष्य के बारे में सोच सकता था, इस पुश्तैनी ज़मीन को लेकर सपने भी बुन सकता था, कि यहाँ छोटा-सा घर बनाऊँगा, आँगन में फलों के पेड़ लगाऊँगा, पेड़ों के साए के नीचे हरी-हरी घास पर बैठा करूँगा। पर अब? अव्वल तो यह ज़मीन का टुकड़ा अभी भी आसानी से मुझे नहीं मिलेगा। घुसपैठिए को इसमें से निकालना ख़ालाजी का घर नहीं है। मैं घूस दे सकता हूँ तो क्या घुसपैठिया घूस नहीं दे सकता, या नहीं देता होगा? भले ही फ़ैसला मेरे हक़ में हो चुका है, वह दस तिकड़में करेगा। पिछले बीस साल में कितने उतार-चढ़ाव आए हैं, कभी फ़ैसला मेरे हक़ में होता तो वह अपील करता, अगर उसके हक़ में होता तो मैं अपील करता, इसी में ज़िन्दगी के बीस साल निकल गए, और अब 73 साल की उम्र में मैं उस पर क्या घर बनाऊँगा? मकान बनाना कौन-सा आसान काम है? और किसे पड़ी है कि मेरी मदद करे? अगर बना भी लूँ तो भी मकान तैयार होते-होते मैं 75 पार कर चुका होऊँगा। मेरे वकील की उम्र इस समय 80 साल की है, और वह बौराया-सा घूमने लगा है। बोलने लगता है तो बोलना बंद ही नहीं करता। उसकी सूझ-बूझ भी शिथिल हो चली है, बैठा-बैठा अपनी धुँधलाई आँखों से शून्य में ताकने लगता है। कहता है उसे पेचिश की पुरानी तकलीफ़ भी है, घुटनों में भी गठिया है। वह आदमी 80 वर्ष की उम्र में इस हालत में पहुँच चुका है, तो इस उम्र तक पहुँचते-पहुँचते मेरी क्या गति होगी? मकान बन भी गया तो मेरे पास ज़िन्दगी के तीन-चार वर्ष बच रहेंगे, क्या इतने-भर के लिए अपनी हड्डियाँ तोड़ता फिरूँ? क्यों नहीं मैं इस पचड़े में से निकल आता? मुझसे ज़्यादा समझदार तो मेरा वह वकील ही है, जिसने अपनी स्थिति को समझ लिया है और मेरे साथ तहसील-कचहरी जाने से इंकार कर दिया है।
“बस, साहिब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, आप मुक़दमा जीत गए हैं, अब ज़मीन पर क़ब्ज़ा लेने का काम आप ख़ुद सम्भालें।” उसने दो टूक कह दिया था।
…यही कुछ सोचते-सोचते, उसने फिर से सिर झटक दिया था। क्या मैं यहाँ तक पहुँचकर किनारा कर जाऊँ? ज़मीन को घुसपैठिए के हाथ सौंप दूँ? यह बुज़दिली नहीं होगी तो क्या होगा? किसी को अपनी ज़मीन मुफ़्त में क्यों हड़पने दूँ? क्या मैं इतना गया-बीता हूँ कि मेरे जीते-जी, कोई आदमी मेरी पुश्तैनी ज़मीन छीन ले जाए और मैं खड़ा देखता रहूँ? और अब तो फ़ैसला हो चुका है, अब तो इसे केवल हल्का-सा धक्का देना बाक़ी है। तहसील के काग़ज़ात मिल जाएँ, इंतकाल की नक़लें मिल जाएँ, फिर रास्ता खुलने लगेगा, मंज़िल नज़र आने लगेगी।
…सोचते-सोचते एक बार फिर उसने अपना सिर झटक दिया। ऐसे मौक़े पहले भी कई बार आ चुके थे। तब भी यही कहा करता था, एक बार फ़ैसला हक़ में हो जाए तो रास्ता साफ़ हो जाएगा। पर क्या बना? बीस साल गुज़र गए, वह अभी भी कचहरियों की ख़ाक छान रहा है।
“…साँप के मुँह में छछूँदर, खाए तो मरे, छोड़े तो अंधा हो। न तो मैं इस पचड़े से निकल सकता हूँ, न ही इसे छोड़ सकता हूँ।”
डिप्टी कमिश्नर दफ़्तर में नहीं था। वही बात हुई। किसी ने बताया कि वह किसी मीटिंग में गया है, कुछ मालूम नहीं कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं।
वह चुपचाप एक बेंच पर जा बैठा, कल ही की तरह सिगरेट सुलगायी और अपने भाग्य को कोसने लगा।
“मैं काम करना नहीं जानता, छोटे-छोटे कामों के लिए ख़ुद भागता फिरता हूँ। ये काम मिलने-मिलाने से होते हैं, ख़ुद मारे-मारे फिरने से नहीं, मैं ख़ुद मुँह बाए कभी तहसील में तो कभी ज़िला कचहरी में धूल फाँकता फिरता हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो दस तरकीबें सोच निकालता। सिफ़ारिश डलवाने से लोगों के बीसियों काम हो जाते हैं और मैं यहाँ मारा-मारा फिर रहा हूँ।”
तब डिप्टी कमिश्नर के चपरासी ने भी कह दिया था कि अब साहिब नहीं आएँगे और दफ़्तर के बाहर, दरख़्वास्तियों के लिए रखा बेंच उठाकर अंदर ले गया था। उधर कचहरी का जमादार बरामदे और आँगन बुहारने लगा था। सारा दिन यों बर्बाद होता देखकर वह मन ही मन तिलमिला उठा था। आग की लपट की तरह एक टीस-सी उसके अंदर उठी थी, हार तो मैं नहीं मानूँगा, मैं भी अपनी ज़मीन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी हठ पकड़ लूँगा, इस काम से चिपक जाऊँगा, ये लोग मुझे कितना ही झिंझोड़ें, मैं छोड़ूँगा नहीं, इसमें अपने दाँत गाड़ दूँगा, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, मैं छोड़ूँगा नहीं…
वह मन-ही-मन जानता था कि मन में से उठने वाला यह आवेग उसकी असमर्थता का ही द्योतक था कि जब भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वह ढिठाई का दामन पकड़ लेता है, इस तरह वह अपने डूबते आत्मविश्वास को धृष्टता द्वारा जीवित रख पाने की कोशिश करता रहता है।
पर उस दिन सुबह, ज़िला कचहरी की ओर जाने से पहले उसकी मनःस्थिति बिल्कुल दूसरी थी। तब वह आश्वस्त महसूस कर रहा था, नहा-धोकर, ताज़ादम घर से निकला था और उसे पता चला था कि डिप्टी कमिश्नर दफ़्तर में मिलेगा, कि वह भला आदमी है, मुंसिफ़-मिज़ाज है। और फिर उसका तो काम भी मामूली-सा है, अगर उससे बात हो गई और उसने हुक्म दे दिया तो पलक मारते ही काम हो जाएगा। शायद इसीलिए जब वह घर से निकला था तो आसपास का दृश्य उसे एक तस्वीर जैसा सुंदर लगा था, जैसे माहौल में से बरसों की धुंध छँट गई हो और विशेष रोशनी-सी चारों ओर छिटक गई हो, एक हल्की-सी झिलमिलाहट, जिसमें एक-एक चीज—नदी का पाट, उस पर बना सफ़ेद डँडहरों वाला पुल, और नदी के किनारे खड़े ऊँचे-ऊँचे भरे-पूरे पेड़, सभी निखर उठे थे। सड़क पर जाती युवतियों के चेहरे खिले-खिले। हर इमारत निखरी-निखरी, सुबह की धूप में नहायी। और इसी मनःस्थिति में वह उस बस में बैठ गया था जो उसे शहर के बाहर दूर, डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर की ओर ले जाने वाली थी।
फिर शहर में से निकल जाने पर, वह बस किसी घने झुरमुट के बीच, स्वच्छ, निर्मल जल के एक नाले के साथ-साथ चली जा रही थी। उसने झाँककर, बस की खिड़की में से बाहर देखा था। एक जगह पर नाले का पाट चौड़ा हो गया था, और पानी की सतह पर बहुत-सी बतखें तैर रही थीं, जिससे नाले के जल में लहरियाँ उठ रही थीं। किनारे पर खड़े बेंत के छोटे-छोटे पेड़ पानी की सतह पर झुके हुए थे और उनका साया जालीदार चादर की तरह पानी की सतह पर थिरक रहा था। अब बस किसी छोटी-सी बस्ती को लाँघ रही थी। बस्ती के छोटे-छोटे बच्चे, नंगे बदन, नाले में डुबकियाँ लगा रहे थे। उसकी नज़र नाले के पार, बस्ती के एक छोटे से घर पर पड़ी जो नाले के किनारे पर ही, लकड़ी के खम्भों पर खड़ा था, उसकी खिड़की में एक सुंदर-सी कश्मीरी लड़की, अपनी छोटी बहिन को सामने बैठाए उसके बालों में कंघी कर रही थी। थोड़ी देर के लिए ही यह दृश्य उसकी आँखों के सामने रहा था और फिर बस आगे बढ़ गई थी। पर उसे देखकर उसके दिल में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई थी… एक छोटा-सा घर तो बन ही सकता है। मन में एक बार निश्चय कर लो तो, जैसे-तैसे, काम पूरा हो ही जाता है। बेंत के पेड़ के नीचे, आँगन में, कुर्सी बिछाकर बैठा करूँगा, पेड़ों की पाँत के नीचे, मैं और मेरी पत्नी घूमने जाया करेंगे। पेड़ों पर से झरते पत्तों के बीच क़दम बढ़ाते हुए, मैं हाथ में छड़ी लेकर चलूँगा, मोटे तले के जूते पहनूँगा, और ठण्डी-ठण्डी हवा गालों को थपथपाया करेगी। ज़िन्दगी-भर की थकान दूर हो जाएगी… मकान बनाना क्या मुश्किल है! क्या मेरी उम्र के लोग काम नहीं करते? वे फ़ैक्टरियाँ चलाते हैं, नई फ़ैक्टरियाँ बनाते हैं, मरते दम तक अपना काम बढ़ाते रहते हैं।
पर अब, ढलती दोपहर में, खचाखच भरी बस में हिचकोले खाता हुआ, बेसुध-सा, शून्य में देखता हुआ, वह घर लौट रहा था। पिंडलियाँ दुख रही थीं और मुँह का ज़ायका कड़वा हो रहा था।
उसे फिर झुँझलाहट हुई अपने पर, अपने वकील पर जिसने ऐन आड़े वक़्त में मुक़दमे पर पीठ फेर ली थी; अपनी सगे-सम्बन्धियों पर, जिनमें से कोई भी हाथ बँटाने के लिए तैयार नहीं था। मैं ही मारा-मारा फिर रहा हूँ। सबसे अधिक उसे अपने पर क्रोध आ रहा था, अपनी अकर्मण्यता पर, अपने दब्बू स्वभाव पर, अपनी असमर्थता पर।
बस में से उतरते ही उसने सीधे अपने वकील के पास जाने का फ़ैसला किया। वह अंदर-ही-अंदर बौखलाया हुआ था। फ़ीस लेते समय तो कोई कसर नहीं छोड़ते, दस की जगह सौ माँगते हैं, और काम के वक़्त पीठ मोड़ लेते हैं। तहसीलों में धक्के खाना क्या मेरा काम है? क्या मैंने तुम्हें उजरत नहीं दी?
कमिश्नरी का बड़ा फाटक लाँघकर वह बाएँ हाथ को मुड़ गया, जहाँ कुछ दूरी पर, अर्जीनवीसों की पाँत बैठती थी। बूढ़ा वकील कुछ मुद्दत से अब यहीं बैठने लगा था। उसने नज़र उठाकर देखा, छोटे-से लकड़ी के खोखे में वह बड़े इत्मीनान से लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसका चौड़ा चेहरा दमक रहा था। और सिर के गिने-चुने बाल बिखरे हुए थे। उसे लगा जैसे बूढ़े वकील ने नया सूट पहन रखा है और उसके काले रंग के जूते चमक रहे हैं।
वह अपने बोझिल पाँव घसीटता, धीरे-धीरे चलता हुआ, वकील के खोखे के सामने जा पहुँचा। बूढ़ा वकील काग़ज़ों पर झुका हुआ था, और एक नोटरी की हैसियत से अर्ज़ियों पर किए गए दस्तख़तों की तसदीक़ कर रहा था, और नीचे, ज़मीन पर खड़ा, अधेड़ उम्र का उसका कारिंदा, हाथ में नोटरी की मोहर उठाए, एक-एक दरख़्वास्त पर दस्तख़त हो जाने पर, ठप्पा लगा रहा था।
“आज भी कुछ काम नहीं हुआ”, खोखे के सामने पहुँचते ही, उसने क़रीब-क़रीब चिल्लाकर कहा। वकील को यों आराम से बैठा देखकर उसका ग़ुस्सा भड़क उठा था। ख़ुद तो कुर्सी पर मज़े से बैठा, दस्तख़तों की तसदीक़ कर रहा है, और पैसे बटोर रहा है, जबकि मैं तहसीलों की धूल फाँक रहा हूँ।
वकील ने सिर उठाया, उसे पहचानते ही मुस्कराया। वकील ने उसका वाक्य सुन लिया था।
“मैंने कहा था ना?” वकील अपनी जानकारी बघारते हुए बोला, “तहसीलों में दस-दस दिन लटकाए रखते हैं। मैं आजिज़ आ गया था, इसीलिए आपसे कह दिया था कि अब मैं यह काम नहीं करूँगा।”
“आप नहीं करेंगे तो क्या मैं तहसीलों की ख़ाक छानता फिरूँगा?” उसने खीझकर कहा।
“यह काम मैं नहीं कर सकता। यह काम ज़मीन के मालिक को ही करना होता है।”
उसका मन हुआ बूढ़े वकील से कहे, बरसों तक तुम इस मुक़दमे की पैरवी करते रहे हो। मैं तुम्हें मुँह-माँगी उजरत देता रहा हूँ, और अब, जब आड़ा वक़्त आया है तो तुम इस काम से किनारा कर रहे हो, और मुझसे कह रहे हो कि ज़मीन के मालिक को ही यह काम करना होता है।
पर उसने अपने को रोक लिया, मन में उठती खीझ को दबा लिया। बल्कि बड़ी संयत, सहज आवाज़ में बोला, “वकील साहिब, आप मुक़दमे के एक-एक नुक्ते को जानते हैं। आपकी कोशिशों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसे छोटा-सा धक्का और देने की ज़रूरत है, और वह आप ही दे सकते हैं।”
पर बूढ़े वकील ने मुँह फेर लिया। उसकी उपेक्षा को देखते हुए वह मन-ही-मन फिर तमक उठा। पर उसकी नज़र वकील के चेहरे पर थी—80 साल का बूढ़ा शून्य में देखे जा रहा था। अपने दम-ख़म के बावजूद वकील की आँखें धुँधला गई थीं, और बैठे-बैठे अपने आप उसका मुँह खुल जाता था। इस आदमी से यह उम्मीद करना कि यह तहसीलों-कचहरियों के चक्कर काटेगा, बड़ी बेइंसाफ़ी-सा लगता था। और अगर काटेगा भी तो कितने दिन तक काट पाएगा?
उसे फिर अपनी निःसहायता का भास हुआ। कोई भी और आदमी नहीं था जो इसका बोझ बाँट सके, उसे साँस तक ले पाने की मोहलत दे सके। बेटे थे तो एक बम्बई में जा बैठा तो दूसरा अम्बाला में, और मैं इस उम्र में श्रीनगर में झख मार रहा हूँ। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। मैं आँखे बंद कर लूँगा तो अपने आप ज़मीन का मसला सुलझाते फिरेंगे।
“वकील साहिब, आप ही इस नाव को पार लगा सकते हैं।” उसने कहना शुरू ही किया था कि वकील झट से बोला, “मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, आप मुझे माफ़ करें, अब यह मेरे बस का नहीं है।”
फिर अपने खोखे की ओर इशारा करते हुए बोला, “आपने देख लिया यह काम कैसा है। यहाँ से मैं अगर एक घंटे के लिए भी उठ जाऊँ तो कोई दूसरा नोटरी मेरी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा।”
फिर क्षीण-सी हँसी हँसते हुए कहने लगा, “सभी इस ताक में बैठे हैं कि कब बूढ़ा मरे और वे उसकी कुर्सी सम्भालें… मैं अपना अड्डा नहीं छोड़ सकता। मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, और यहाँ पर बिना भाग-दौड़ के मुझे दो पैसे मिल जाते हैं, बुढ़ापे में यही काम कर सकता हूँ।”
“मुश्किल काम तो हो गया, वकील साहिब, अब तो छोटा-सा काम बाक़ी है।”
“छोटा-सा काम बाक़ी है?” वकील तुनककर बोला, “ज़मीन का क़ब्ज़ा हासिल करना क्या छोटा-सा काम है? यह सबसे मुश्किल काम है।”
“सुनिए, वकील साहिब…” उसने कहना शुरू ही किया था कि वकील ने हाथ जोड़ दिए, “आप मुझे माफ़ करें, मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा…”
सहसा, वकील के चेहरे की ओर देखते हुए एक बात उसके दिमाग़ में कौंध गई। वह ठिठक गया, और कुछ देर तक ठिठका खड़ा रहा, फिर वकील से बोला, “नहीं, वकील साहिब, मैं तो कुछ और ही कहने जा रहा था।”
“कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं?”
वह क्षण-भर के लिए फिर सोच में पड़ गया, फिर छट से बोला, “अगर आप ज़मीन पर क़ब्ज़ा हासिल करने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, तो क़ब्ज़ा मिलने पर मैं आपको ज़मीन का एक-तिहाई हिस्सा दे दूँगा।”
उसने आँख उठाकर बूढ़े वकील की ओर देखा। वकील जैसे सकते में आ गया था, और उसका मुँह खुलकर लटक गया था।
“पर इस शर्त पर कि अब इस काम में मैं ख़ुद कुछ नहीं करूँगा। सब काम आप ही करेंगे।” वह कहता जा रहा था।
“मैंने तो अर्ज़ किया न, मेरी मजबूरी है…” बूढ़ा वकील बुदबुदाया।
“आप सोच लीजिए। एक तिहाई ज़मीन का मतलब है करीब चार लाख रुपए…”
यह विचार उसे अचानक ही सूझ गया था, मानो जैसे कौंध गया हो। अपनी विवशता के कारण रहा हो, या दबी-कुचली व्यवहार-कुशलता का कोई अधमरा अंकुर सहसा फूट निकला हो। पर इससे उसका ज़ेहन खुल-सा गया था।
“आप नहीं कर सकते तो मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता। आप किसी अच्छे वकील का नाम तो सुझा सकते हैं जो दौड़-धूप कर सकता हो। मुक़दमे की स्थिति आप उसे समझा सकते हैं”, उसने अपनी व्यवहार-कुशलता का एक और तीर छोड़ते हुए कहा, “आप मुक़दमे को यहाँ तक ले आए, यही बहुत बड़ी बात है।”
उसने बूढ़े वकील के चेहरे की ओर फिर से देखा। बूढ़े वकील का मुँह अभी भी खुला हुआ था और वह उसकी ओर एकटक देखे जा रहा था।
“अब कोई वकील ही यह काम करेगा…”
बूढ़े वकील की आँखों में हल्की-सी चमक आ गई थी और उसका मुँह बंद हो गया था।
“मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि केस की सारी मालूमात आपको है। अपना सुझाव सबसे पहले आपके सामने रखना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अदालत का फ़ैसला हमारे हक़ में हो चुका है। अब केवल क़ब्ज़ा लेना बाक़ी है…”
अपनी बात का असर बूढ़े वकील के चेहरे पर होता देखकर, वह मन-ही-मन बुदबुदाया, “लगता है तीर निशाने पर बैठा है।”
“लेकिन मैं अपने पल्लू से अब और कुछ नहीं दूँगा। न पैसा, न फ़ीस, न मुआवज़ा, कुछ भी नहीं। बस, एक-तिहाई ज़मीन आपकी होगी, और शेष मेरी…”
बोलते हुए उसे लगा जैसे उसके शरीर में ताक़त लौट आयी है, और आत्मविश्वास लहराने लगा है। उसे लगा जैसे अगर वह इस वक़्त चाहे तो भाषण दे सकता है।
“पटवारी, तहसीलदार, घुसपैठिया, जिस किसी को कुछ देना होगा तो आप ही देंगे…”
फिर बड़े ड्रामाई अंदाज़ में वह चलने को हुआ, और धीरे-धीरे बड़े फाटक की ओर क़दम बढ़ाने लगा।
“अपना फ़ैसला आज शाम तक मुझे बता दें”, फिर, पहले से भी ज़्यादा ड्रामाई अंदाज़ में बोला, “अगर मंज़ूर हो तो मैं अभी मुआहिदे पर दस्तख़त करने के लिए तैयार हूँ।”
और बिना उत्तर का इंतज़ार किए, बड़े फाटक की ओर बढ़ गया।
दूसरे दिन, अपनी मृत्यु के कुछ ही देर पहले, वह पार्क में, एक बेंच पर बैठा, हल्की-हल्की धूप का आनंद ले रहा था और पिछले दिनों की थकान उतार रहा था। वह मन-ही-मन बड़ा आश्वस्त था कि उसे एक बहुत बड़े बोझ से छुटकारा मिल गया है। अब वह चैन से बैठ सकता है और फिर से भविष्य के सपने बुन सकता है।
इस प्रस्ताव ने दोनों बूढ़ों की भूमिका बदल दी थी। जिस समय वह धूप में बैठा अधमुँदी आखों से हरी-हरी घास पर चमकते ओस के कण देख रहा था, उसी समय तहसील की ओर जाने वाली खचाखच भरी बस में, डँडहरे को पकड़कर खड़ा वकील अपना घर बनाने के मनसूबे बाँध रहा था। दिल में रह-रहकर गुदगुदी-सी उठती थी। ज़िन्दगी-भर किराए के मकान में, तीसरी मंज़िल पर टँगा रहा हूँ। किसी से कहते भी शर्म आती है कि सारी उम्र काम करने के बाद भी अपना घर तक नहीं बना पाया। बेटे बड़े हो गए हैं और दिन-रात शिकायत करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है? …इधर खुली ज़मीन होगी, छोटा-सा आँगन होगा, दो-तीन पेड़ फलों के लगा लेंगे, छोटी-सी फुलवाड़ी बना लेंगे। ज़िन्दगी के बचे-खुचे सालों में, कम-से-कम रहने को तो खुली जगह होगी, सँकरी गली में, तीसरी मंज़िल पर लटके तो नहीं रहेंगे… एक स्फूर्ति की लहर, पुलकन-सी, एक झुरझुरी-सी उसके बदन में उठी और सरसराती हुई, सीधी, रीढ़ की हड्डी के रास्ते सिर तक जा पहुँची। खुली ज़मीन का एक टुकड़ा, लाखों की लागत का, बैठे-बिठाए, मुफ़्त में मिल जाएगा, न हींग लगे, न फिटकरी। अच्छा हुआ जो लिखा-पढ़ी भी हो गई, मुवक्किल को दोबारा सोचने का मौक़ा ही नहीं मिला।
इस गुदगुदी में वह बस पर चढ़ा था। पर कुछ फ़ासला तय कर चुकने पर, बस में खड़े-खड़े बूढ़े वकील की कमर दुखने लगी थी। अस्सी साल के बूढ़े के लिए बस के हिचकोलों में अपना संतुलन बनाए रखना कठिन हो रहा था। दो बार वह गिरते-गिरते बचा था। एक बार तो वह, नीचे सीट पर बैठी एक युवती की गोद में जा गिरा था, जिस पर आसपास के लोग ठहाका मारकर हँस दिए थे। पाँव बार-बार लड़खड़ा जाते थे, पर मन में गुदगुदी बराबर बनी हुई थी।
पर कुछ ही देर बाद, बस में खड़े रहने के कारण, घुटनों में दर्द अब बढ़ेगा। तहसील अभी दूर है और वहाँ पहुँचते-पहुँचते मैं परेशान हो उठूँगा। दर्द बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद उसे लगने लगा जैसे किसी जंतु ने अपने दाँत उसके शरीर में गाड़ दिए, और उसे झिंझोड़ने लगा है। न जाने तहसील तक पहुँचने-पहुँचते मेरी क्या हालत होगी? …बैठे-बिठाए मुसीबत मोल ले ली। जाए भाड़ में ज़मीन का मालिक। और वह जहाँ पर खड़ा था, वहीं घुटने पकड़कर बस के फ़र्श पर, हाय-हाय करता बैठ गया।
उस समय बस, उस बस्ती को पार कर रही थी, जहाँ बेंत के पेड़ों के झुरमुट के बीच, नाले के किनारे-किनारे सड़क चलती जा रही थी, और जहाँ पानी की सतह पर लहरियाँ बनाती हुई, बतखें आज भी तैर रही थीं।
उधर, पार्क के बेंच पर बैठा ज़मीन का मालिक, थकान दूर हो जाने पर, धीरे-धीरे ऊँघने लगा था, उसकी मौत को कुछ ही मिनट बाक़ी रह गए थे। वह अभी भी आश्वस्त महसूस कर रहा था, चलो, इस सारी चख-चख और फ़ज़ीहत में से निकल आया हूँ। उसे यह सोचकर सुखद-सा अनुभव हुआ कि वह आराम से बेंच पर बैठा सुस्ता रहा है जबकि वकील इस समय तहसील में ज़मीन के काग़ज़ निकलवाने के लिए भटक रहा है। …पर ज़मीन का ध्यान आते ही उसके मन को धक्का-सा लगा। सहसा ही वह चौंककर उठ बैठा। यह मैं क्या कर बैठा हूँ? एक तिहाई ज़मीन दे दी? अदालत का फ़ैसला तो मेरे हक़ में हो चुका है। अब तो केवल क़ब्ज़ा लेना बाक़ी था। ज़मीन तो मुझे मिल ही जाती। लाखों की ज़मीन उसके हवाले कर दी और लिखत भी दे दी। कहाँ तो वकील को ज़्यादा-से-ज़्यादा पाँच सौ-हज़ार की फ़ीस दिया करता था, वह भी चौथे-पाँचवें महीने, और कहाँ एक-तिहाई ज़मीन ही दे दी। लूटकर ले गया, बैठे-बिठाए लूटकर ले गया। उसके मन में चीख-सी उठी। यह मैं क्या कर बैठा हूँ? न किसी से पूछा, न बात की। देना ही था तो एकमुश्त कुछ रक़म देने का वादा कर देता। अपनी ज़मीन कौन देता है? बैठे-बिठाए मैंने काग़ज़ पर—वह भी स्टाम्प पेपर पर दस्तख़त कर दिए। यह मैं क्या कर बैठा हूँ? और स्टाम्प पेपर की तस्वीर आँखों के सामने खिंच गई। तभी कहीं से ज़ोर का धक्का आया और दर्द-सा उठा, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और वह बेंच पर से लुढ़ककर, नीचे, ओस से सनी, हरी-हरी घास पर, औंधे मुँह जा गिरा।
भीष्म साहनी की कहानी 'अमृतसर आ गया है'