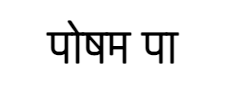भारी ढक्कन से ढँके दीपक के समान आकाश में बिजली बुझ गयी थी। सन्ध्या से ही हवा बादलों की तह-पर-तह जमाने में व्यस्त रही और अब वे इतने सघन हो उठे कि रात के छायारूपों के उपयुक्त ही एक अखण्ड, पर अपनी आर्द्रता से रिसती हुई काली शिला की छत बन गए।
मेरा मन भी बुझा-बुझा-सा हो रहा था। मैं अपने पढ़ने-लिखने के बाहर वाले छोटे कमरे में मेज़ पर सिर रखकर दर्द भुलाने की असफल चेष्टा कर रही थी। छात्रावास में टाइफ़ाइड में पड़ी सुदूर दक्षिण की एक बालिका का मुख मेरी बन्द पलकों में किसी फ़ोटो के इंलार्जमेंट समान बढ़ता चला जाता था। उसके साधारण स्थिति वाले माता-पिता इतना रुपया किस प्रकार पाते कि उसे देखने आ सकते। उसके लिए मन जैसे-जैसे चिन्ताकुल होने लगा, वैसे-वैसे अपने ऊपर झल्लाहट बढ़ने लगी।
जब मेरा शरीर इतना निकम्मा था कि इनके सुख-दुःख में दो-चार रात जागना भी सहज नहीं, तब किस बूते पर मैंने इन बालिकाओं को उनकी माताओं से इतनी दूर ला रखा है? जब अभी तक मनुष्य बनने की स्वयं मेरी ही साधना पूर्ण नहीं हुई, तब इन बालिकाओं को मनुष्य बनाने का भार लेने का मुझे हौसला कैसे हुआ? ऐसे दम्भ को अक्षम्य अपराधों की कोटि में ही स्थान मिलना चाहिए। सहसा बाहर बरामदे में किसी की पग-ध्वनि ने मेरी विचार-शृंखला भंग कर दी।
दो-चार मिनट किसी के पुकारने की प्रतीक्षा करके पूछना ही पड़ा— “कौन?”
उत्तर में एक सुडौल गोरे हाथ ने कुछ बढ़कर परदे को हिला-सा दिया। एक सभीत स्त्री-कण्ठ ने रुक-रुककर प्रश्न किया— “क्या भीतर आ सकती हूँ?”
“आइए”—कहते समय मेरे स्वर में ऐसी उदासीन शिष्टता थी कि आने वाली के पैर बाहर एक बार ठिठके-से रहे; पर क्षण-भर ही, क्योंकि दूसरे क्षण ही वह नीले परदे की पार्श्वभूमि पर एक रंगीन-चित्र-सा बन गयी।
गहरे काही रंग की पतली ऊनी चादर में समा न सकने के कारण वर्षा की नन्हीं-नन्हीं बूँदें ऊपर ही जड़ी-सी थीं, जो बिजली के आलोक में हीरे के चूर-सी झिलमिलाने लगीं। चादर उतारकर जब वह मेरी दृष्टि का अनुसरण करती हुई सामने की कुर्सी पर बैठ गयी, तब मेरी कुछ विस्मय और कुछ जिज्ञासा भरी दृष्टि उस मुख की रेखा-रेखा में, न जाने किस शब्दहीन उत्तर की खोज में भटकने लगी। आँखों के आस-पास लटकती हुई दो-तीन छोटी-छोटी लटों के छोरों में हिलती हुई पानी की बूँदें पारे-सी जान पड़ती थी। सफ़ेद साड़ी के कुछ धबीले बैंजनी किनारे से घिरा मुख सुडौल गोरा; पर बहुत मुरछाया हुआ-सा लगा। नाक के अग्रभाग की लाली हाल ही में पोंछे गए आँसुओं की सूचना दे रही थी—पलकों की कोरें भी शायद रोने से ही कुछ-कुछ सूज आयी थीं, जिनसे उनकी मर्मस्पर्शी व्यथा और भी गहरी हो उठी थी। ओंठ इतने सूख रहे थे कि उन्हें आर्द्र करने का प्रत्येक प्रयास अपनी एकरसता में भी एक नयी थकान का आभास देता जाता था; मैं स्वयं बहुत क्लान्त थी, इसी से उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा में रुकी रही। परन्तु जब उसने अपना सिर और अधिक नीचा कर लिया और आँख से ढुलका हुआ एक आँसू उसकी गोद में गिरने से पहले प्रकाश में एक उजली रेखा-सा चमक गया, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे सामने बैठी हुई यह स्त्री न जाने कौन-सी व्यथा मुझे सुनाने आयी है। इतनी घिरी घटा और बूँदाबाँदी में इसका घर से निकलना ही प्रमाणित किए देता है कि इसकी आवश्यकता कल तक भी नहीं टाली जा सकती थी।
मैंने कुछ उनींदे भाव से कोई असंख्य बार पूछा हुआ और अति परिचय से पुराना प्रश्न ही पूछ लिया होगा, परन्तु ‘मुझे कोई काम दीजिए’ में उत्तर पाकर मैं मानो जागकर सतर्क हो बैठी। काम और योग्यता सम्बन्धी प्रश्न आवश्यक होने पर भी उस स्थिति के लिए निष्ठुर जान पड़े। मेरी कठिनाई का समाधान उसने स्वयं ही कर दिया। वह हिन्दी जानती है… ‘गाना भी’ कहने के पहले उसका सम्पूर्ण शरीर संकुचित हो उठा और कहने के उपरान्त स्फीत होता जान पड़ा, मानो कोई कठिन काम समाप्त कर लिया हो।
कथा और आगे बढ़ी। उनके पति डेढ़ वर्ष से बीमार हैं… दवा-दारू में सब कुछ स्वाहा हो चुका है। गहने के नाम से उसकी उँगली में चार माशे भर सोने का एक छल्ला शेष है। पति का एकमात्र उपहार होने के कारण इसे बेचने का विचार ही उसे क्लान्त कर देता है और बेचकर भी कै दिन चलेगा… यदि कोई काम न मिल सका तो वह स्वयं भूखी रहकर मरने से भी नहीं डरती पर… और उसका गला भर आया। पलकों की कोर तक आए हुए आँसुओं को भी रोक लेने का उसे अभ्यास था। इसी से जिस वेग से उसका शरीर बेंत के समान काँप उठा था, उससे मात्रा में कुछ अधिक संयम ने आँखों की सजल निस्तब्धता को पिघलने नहीं दिया।
सान्त्वना-सूचक कोई उपयुक्त शब्द मुझे खोजने पर भी नहीं मिल सका और तब उसके माता-पिता, सास-ससुर आदि के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट कर मैं अपने आवेग को छिपाने लगी। स्त्री का सम्पूर्ण शरीर फिर पहले के समान ही संकुचित हो उठा—एक हल्की कम्पन लिए हुए शब्दों ने मुझे चौंका-सा दिया। ससुराल वाले रुष्ट हैं—वे उसे घर ले जाने को राज़ी नहीं और पति को अकेले जाना स्वीकार नहीं। विवाह के उपरान्त माँ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उससे रुपया लेने से मृत्यु अच्छी है।
इतनी टीका के उपरान्त मैंने मूल तत्त्व का सूत्र पकड़ पाया। वह पतित कही जाने वाली माँ की पुत्री है और बिना समाज के प्रवेश-पत्र के ही साध्वी स्त्रियों के मन्दिर में प्रवेश करना चाहती थी।
उसे पता नहीं कि समाज के पास वह जादू की छड़ी है, जिससे छूकर वह जिस स्त्री को सती कह देता है, केवल वही सती का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। जिसे समाज ने एक बार कुलवधुओं की पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया, उसे जन्म-जन्मान्तर तक अपनी सभी भावी पीढ़ियों के साथ बाहर खड़ा रहने को ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान समझना चाहिए।
और फिर समाज ने उन्हें क्या छोटा-मोटा काम दिया है! भगवान् के विराट् रूप के समान ही मनुष्य के विराट् रूप की अर्चना का अधिकार इन्हीं को प्राप्त है; परन्तु जब यह अपनी दुर्बुद्धि से अनुशासन भंग कर देती हैं, तब इनका अपराध अक्षम्य हो उठता है। इन्हें जानना ही चाहिए कि जिसने ऊँचे स्वर्ग की सृष्टि की है, उसी ने नीचे पाताल की रचना भी की है। यदि पाताल के सब जीव-जन्तु स्वर्ग की ओर दौड़ पड़ें, तो सृष्टि एक दिन भी न चले। अपने इच्छानुसार ही जीवन को बदलकर यह समाज में जो एक अव्यवस्था उत्पन्न कर रही हैं, उसे रोकने के लिए इन्हें दण्ड देना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो उठता है, नहीं तो समाज की इन पर कुछ ममता नहीं। भला किसे अपनी सृष्टि का मोह नहीं होता! समाज इन्हें न जाने कितने दीर्घकाल से, कितने ही उपायों के द्वारा समझाता आ रहा है कि यह माता, पुत्री, पत्नी आदि त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित जीवनमुक्त नारी-मात्र हैं और इनकी इसी मुक्ति से समाज का कल्याण बँधा हुआ है। फिर भी यदि यह अपने गुरु कर्त्तव्य से च्युत होकर पत्नीत्व, मातृत्व आदि सम्बन्धों को चुराती फिरें, तो समाज चुरायी हुई वस्तु पर इनका स्वत्व स्वीकार करके क्या अपना विधान ही मिथ्या कर दे?
पत्नीत्व की चोरी करने वाली वह अबोध स्त्री अवश्य ही समाज के जटिल नीतिशास्त्र को समझने में असमर्थ रही, तभी तो उसकी जिज्ञासा भरी दृष्टि मेरे मुख पर स्थिर होकर मानो बड़े करुण भाव से बार-बार पूछने लगी— “क्या मैं पवित्र नहीं हूँ?”
एक ओर यह स्त्री है जिसकी माता को माता बनने का अधिकार ही नहीं दिया गया था और दूसरी ओर मैं हूँ जिसकी माता, नानी, परनानी, दादी, परदादी और उसकी भी पूर्वजाएँ अपने पतियों का चरणोदक ले-लेकर और उनमें से कई जीवित ही अग्निपथ पार करके अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी पतिव्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुकी हैं। मैं अनेकों से पूजनीया माँ और आदरणीया बहिन का सम्बोधन पाती रहती हूँ; किन्तू इसे कौन अभागा माँ-बहिन कहकर अपवित्र बनेगा? और वह जानना चाहती है अपने अपवित्र माने जाने का कारण? यह अपने विद्रोही पति के साथ सती ही क्यों न हो जावे, परन्तु इसके रक्त के अणु-अणु में व्याप्त मलिन संस्कार कैसे धुल सकेगा? स्वेच्छाचार से उत्पन्न यह पवित्रता की साधना उस शूद्र की तपस्या के समान ही बेचारे समाज की वर्ण-व्यवस्था का नाश कर रही है, जिसका मस्तक काटने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम दौड़ पड़े थे।
उसे घर भेजने का प्रबन्ध कर मैं जब फाटक से लौटी, तब धरती और मेरे पैर लोहा-चुम्बक बन रहे थे। उस रात कितनी देर तक मैं इसी समस्या में उलझी रही, यह याद नहीं आता; पर कोई समाधान न निकल सका। अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए भी वह दान नहीं स्वीकार करेगी… और काम देने की बात स्मरण कर मेरे ओंठों में एक व्यंग की हँसी आए बिना न रह सकी। वह क्या जाने कि उसकी उपस्थिति क्या-क्या अनर्थ कर सकती है!
फिर दो दिन प्रयत्न करने पर भी जब उसका कहीं प्रबन्ध न हो सका, तब मैंने क्या किया, इसकी कथा मनोविज्ञान सम्बन्धी मेरे अज्ञान को प्रकट करती है। कभी कोई ऐसा लेख नक़ल करने के लिए दे दिया, जिसके पृष्ठों का कोई उपयोग ही शेष न रहा था। कभी कोई ऐसा पत्र लिखवा दिया, जिससे रद्दी काग़ज़ों की टोकरी का ही गौरव बढ़ता था; पर जब उसकी दृष्टि संकोच के भार से और अधिक नत हो गयी, कण्ठ और अधिक कुण्ठित जान पड़ने लगा, तब मैंने समझा कि उसने इस काम के अभिनय के भीतर तक देख लिया है। मुझे उसके काम की आवश्यकता नहीं, यह जब उसका रोम-रोम जानने लगा, तब इस अभिनय को और चलाने का मेरा साहस भी समाप्त हो आया।
फिर कुछ दिनों तक उसका कोई समाचार ही नहीं मिल सका। कदाचित् पति का रोग अधिक भयंकर हो उठा होगा। इस बीच में केवल एक बार उसने सहायता की याचना की, जिससे मैंने समझ लिया कि मेरी सहानुभूति को सत्य रूप में ही उसने स्वीकार किया है।
दिन के सप्ताह और सप्ताह के महीने बन जाने पर एक दिन उसकी किसी परिचित स्त्री से मुझे इस करुण-कथा का जो उपसंहार ज्ञात हुआ, वह तो सुना-सुनाया कहा जाएगा; पर उसने मेरे मर्म को जितना स्पर्श किया, उतना कोई और घटना नहीं कर सकी।
उस अभागी स्त्री की इतनी एकान्त साधना भी उसके पति को न बचा सकी। अंतिम क्षणों में पुत्र का मुख देखने जो पिता आए थे, उन्होंने अनाहार से दुर्बल, अनेक रातों से जागी वधू की ओर भूलकर भी दृष्टिपात नहीं किया। कदाचित् उनके मन में भी यही धारणा रही हो कि उसी अनाचारिणी के कारण उनके पुत्र को जीवन से हाथ धोना पड़ा है।
पड़ोसिनों में से जब किसी ने आकर उसकी बेहोशी दूर की, तब सब उसके मृत पति को ले जा चुके थे। रात-भर वह उसी प्रकार बैठी रही; परन्तु सबेरे ससुर को जाने के लिए सामान ठीक करते देख उसकी चेतना लौटी। आँचल से आँखें पोंछकर जब उसने किवाड़ की ओट से प्रश्न किया— “कै बजे चलना है” तो मानो ससुर-देवता पर गाज गिरी। प्रथम आघात सहकर जब उनमें बोलने की शक्ति लौटी, तब उन्होंने भी क्रूरतम प्रहार किया। कहा— “जो लेकर अपने घर से निकली थी, वही लेकर भलमनसाहत से अपनी माँ के पास लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमें बुरी तरह पेश आना पड़ेगा। हमारे कुल में दाग़ लगाकर भी क्या तुम्हें सन्तोष नहीं हुआ?”
स्त्री ने क्रोध नहीं किया, मान-अपमान का विचार नहीं किया। जिस घर पर उसका न्यायोचित अधिकार था, उसी में पग-भर भूमि की भीख माँगने के लिए आँचल फैलाकर दीनता से कहा— “घर में कई नौकर-चाकर हैं। मेरे लिए दो मुट्ठी आटा भारी न होगा। मैं भी आपकी सेवा करती हुई पड़ी रहूँगी।”
किन्तु ससुर का उत्तर लज्जा को भी लज्जित कर देने वाला था।
मुझ तक यह समाचार विलम्ब से पहुँच सका। खोज करने पर किसी ने बताया वह विधवा-आश्रम चली गयी है; किसी ने कहा, वह माँ के पास लौट गयी।
धीरे-धीरे समय जब उसकी स्मृति को फीका कर चुका था, तब अचानक एक मैले-कुचैले लिफ़ाफ़े ने फिर सब कुछ सजीव कर दिया। वह अच्छी है, मुझे नहीं भूली है; पर और कष्ट नहीं देना चाहती। सिलाई-बुनाई आदि के द्वारा उसे कुछ मिल ही जाता है; जब नहीं मिलेगा, तब मुझसे माँगने में उसे संकोच न होगा।
और भी पूछा है, ऐसी स्त्रियों को जीविका के साधन सिखाने के लिए जो आश्रम मैं खोलना चाहती थी, उसे कब खोलूँगी।
और मैं अपने मन से प्रश्न कर रही हूँ, ‘क्या तुझे आज भी आभिजात्य का गर्व है? क्या तुझे आज भी समाज द्वारा मिले भलाई-बुराई के प्रमाण-पत्रों पर विश्वास है?’
महादेवी वर्मा का लेख 'स्त्री के अर्थ-स्वातंत्रय का प्रश्न'