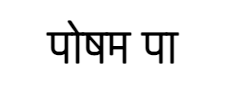तुम कहती हो
“कहते हो.. प्यार करते हो.. तो मान लेती हूँ”
मगर, क्यों मान लेती हो?
आख़िर, क्यों मान लेती हो?
पृथ्वी तो नहीं मानती अपने गुरुत्व को
जब तक कोई
ज़मीन से अपनी जड़ें छुड़ाए
पंख फैलाए
पहुँच ना जाए
उतने ही असीम और अथाह आकाश में
और फिर लौट ना आए
उसी गति के साथ
जिस गति से उसने धरती को छोड़ा था
बरसात तो नहीं मानती अपने घनत्व को
जब तक
हर छतरी, हर छत
हर ओट, हर दरख़्त
विफल ना सिद्ध हो जाए
उसे शुष्क रख पाने में
जिसे वो बरसात भिगोना चाहती है
खुशबू तो नहीं मानती अपनी अस्तित्व को
जब तक
किसी एक की साँसों से गुज़र
दूसरे के सीने पे पसर
दोनों के मन में एक असमंजस ना पैदा कर दे
कि साँसें किसकी हैं
और सीना किसका
फिर तुम इतनी सरलता से कैसे कह देती हो कि
“कहते हो.. प्यार करते हो.. तो मान लेती हूँ”
राह तो नहीं मानती अपने पड़ाव को
जब तक
सिलसिलों के चलन में
काफ़िलों के आवागमन में
उस पड़ाव तक पहुँचते ही
किसी मुसाफिर की उसकी मंज़िल तक पहुँचने की
सम्भावना तो बढ़ जाए
किन्तु इच्छा ख़त्म ना हो जाए
नदिया तो नहीं मानती अपने बहाव को
जब तक
पर्वतों को तोड़कर
सीमाओं को छोड़कर
उस वेग से ना जा गिरे समन्दर के सीने पर,
कि घाव कर दे
और उस घाव से रिस्ता समन्दर का ह्रदय
याद ना कर बैठे उस नदी को
जो सागर सृजन के बाद उसमें सर्वप्रथम सम्मलित हुई थी
किसी पुरातन प्रथम प्रेम की तरह
छाँव तो नहीं मानती अपने फैलाव को
जब तक
शाखों के गुटों ने
पत्तों के झुरमुटों ने
मुँह ना चिढ़ा दिया हो
ईर्ष्या में जलते उस सूरज को
जो उस छाँव तले, आँखें मूँदे, सुस्ताते राही के
सारे स्वप्न अपनी धूप में जला देना चाहता है
फिर तुम इतनी सहजता से कैसे कह देती हो कि
“कहते हो.. प्यार करते हो.. तो मान लेती हूँ”
रात तो नहीं मानती अपने अन्धकार को
जब तक
प्रेम में मगन
दो बदन
जो खोजते हों खुद को
एक दूसरे में,
उन्हें कुछ मिलें
तो केवल दो परछाईयाँ
जिनका आकार अथवा आकृति उस अँधेरे में देख पाना
असम्भव हो
मदिरा तो नहीं मानती अपने ख़ुमार को
जब तक
प्यास भी एक भूख ना हो जाए
मदिरा भी माशूक ना हो जाए
जिसका अक्स भुलाने को वो झाँक पड़ा था प्यालों में
घुटता था उसका दम जिसके बालों के जालों में
मदिरा भी बूँद-बूँद वही मौत ना देने लग जाए
जो उस माशूक ने मुक़र्रर की थी
सोच तो नहीं मानती अपने विस्तार को
जब तक
सदियों के प्रयत्नों से
जाने किन-किन जतनों से
तुम्हारा वर्तमान एक रास्ता ना बना दे
उजले भविष्य की ओर
जो आता तो तुम्हारे भूतकाल से ही हो
किन्तु वहाँ से आता प्रतीत ना होता हो
फिर तुम आखिर कैसे कह देती हो कि
“कहते हो.. प्यार करते हो.. तो मान लेती हूँ”
देह तो नहीं मानती अपने निवास को
जब तक
देख ना लें
तुम और मैं
रंग बिरंगी दीवारें
चिकने फर्श
पानी चूती छत
चहकती मुंडेर
हरा सा आँगन
सूखा सा पीपल
दीमक खाए किवाड़
सब कुछ..
इन्हीं दो शरीरों में..
मृत्यु तो नहीं मानती अपने ग्रास को
जब तक
पाँव में छन-छन किए
कृष्ण-रुपी मन लिए
जैसे राधा दौड़ आती है मुरली की तान पर
कृष्ण तक
वैसे ही वह देह जाने किस मोह में भ्रमित हो
अनभिज्ञ सी
पहुँच ना जाए उस स्थान पर
जहाँ उसका अन्त
निश्चित है
आत्मा तो नहीं मानती अपने निकास को
जब तक
सोती सी एक जाग में
चिता से उठती आग में
जल ना जाएँ देह के संग
वे सारी रातें जिनमें एक अकेलापन किसी का इंतज़ार किया करता था
वे सारे अनुभव जो आँखों से अश्रु बन-बन निकलते थे
वे सारी भावनाएँ जिन्हें जीवित रहते पूर्ण रूप से
ना कभी समझ पाए, ना कभी मान पाए
तुम आखिर क्या मानकर कह देती हो कि
“कहते हो.. प्यार करते हो.. तो मान लेती हूँ”
देखो ऐसे ना मान लिया करो बातें मेरी
यूँ ही..
हाँ यह बात और है
कि जो कह दिया है
उसे अर्थहीन
अथवा असत्य
मैं कभी होने नहीं दूँगा…।
नोट: इस कविता का एक पाठ यहाँ देखा जा सकता है।