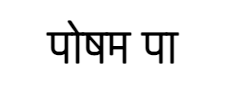आदमी, शरीर से ही नहीं थकता, मन से भी थकता है। मन से थका हुआ आदमी सहानुभूति का विषय है, शरीर से थका हुआ आदमी श्रम के उल्लास का। श्रम के उल्लास में पूर्णता का हर्ष है, पारिश्रमिक का सुख है। मन की थकान एक खण्डित अवस्था है। किंकर्तव्यविमूढ़ अवस्था। मन से थका हुआ आदमी, संवाद चाहता है। मन का भार किसी की पीठ पर लदा कोई बोझ नहीं है, जिसे एक नियत दूरी पर रखकर निजात पायी जा सके। मन का भार संवाद की पूर्णता में ही हल्का होता है।
बुरी चीज़ें, बुरा दौर तो लौटता रहता है जीवन में, अच्छी चीज़ें और अच्छा दौर भी लौटता है। हमें इंतज़ार के इल्म को सीखना चाहिए। संवादहीनता की अवस्था में मौन, सबसे सुंदर भाषा है। मौन, अध्यात्म की भाषा है। मौन, शोक की अभिव्यंजना है। मौन, करुणा की अभिव्यक्ति है। मौन में गुम्फित है धैर्य। मौन, सच के स्वीकार की भी अवस्था है। अज्ञेय यूँ ही नहीं लिखते—
“कहा सागर ने : चुप रहो!
मैं अपनी अबाधता जैसे सहता हूँ, अपनी मर्यादा तुम सहो।
जिसे बाँध तुम नहीं सकते
उसमें अखिन्न मन बहो।
मौन भी अभिव्यंजना है : जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो।”
***
मेरी बालकनी से एक लैम्प-पोस्ट दिखती है। यह हॉस्टल के मुख्य द्वार के सामने वाली लैम्प-पोस्ट है, जिसे मैं बीती कई रातों से देख रहा हूँ। वह लगातार जलने की असफल कोशिश कर रही है। आज शाम हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद की भीगी सड़क और आस-पास खड़े वृक्ष के पत्तों पर उसकी रौशनी एक पल को चमकती है और दूसरे ही पल फिसलकर ग़ायब हो जाती है।
पिछले कुछ सालों में कितना कुछ है जो ग़ायब हो चुका है। पीली रौशनी वाले लैम्प-पोस्ट हों या फ़िर पीछे लौटने का रास्ता। घर भी कितना पीछे छूट गया है। लौटकर भी कहाँ लौट पाता हूँ, कितना अस्थायी होता है, वहाँ लौटना अब! निर्मल वर्मा के उपन्यास ‘वे दिन’ का एक पात्र, इंडी कहता है : “मैं सोचता हूँ, एक उम्र के बाद तुम घर वापस नहीं जा सकते। तुम उसी घर में वापस नहीं जा सकते, जैसे जब तुमने उसे छोड़ा था।”
हाँ, यही सच है। कहीं भी लौटने की एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद आप नहीं लौट सकते वहाँ, उसी जगह, उसी तरह। स्मृतियाँ पेड़ से चिपकी पत्तियों की तरह फड़फड़ाती हैं। पत्ता गिरता है, एक और रास्ता बंद हो जाता है।
रात की निस्तब्धता में अनायास ही कितना कुछ सुनायी देता है। पत्तों की हरहराहट, मानो हवा ने कोई शरारत की हो। घड़ी की टिक-टिक, मानो उसे अपनी उपस्थिति का ख़्याल रात में ही आता है। कभी-कभी, मुझे रात से बेहतर कुछ नहीं लगता। रात से ज़्यादा रचनात्मक कुछ नहीं लगता। तमाम रंग-ओ-बू रात की सृजनात्मकता का ही तो प्रतिफलन है।
रोज़ एक नयी सुबह तैयार करने में, हमारी प्रकृति रात-भर जुटी रहती है। मैं जब भी उसकी इस क्रियाशीलता को रात के अँधेरे में महसूस करता हूँ, कृतज्ञता से भर उठता हूँ।
***
कभी-कभी सोचता हूँ; कल को यदि मैं न रहूँ, तो क्या कोई ऐसा होगा, जो उन जगहों पर कभी-कभी जाकर बैठ जाया करे, जहाँ मैं बदस्तूर जाता रहा हूँ और जिन जगहों से मेरा बहुत लगाव रहा है। किसे इतनी फ़ुर्सत है जो खण्डहर के अवशेषों में अतीत के चिह्न ढूँढे? कितनी तेज़ी से बदल रहा है समय का वर्तमान! कितनी तेज़ी से बदल रही हैं हमारी भावनाएँ! खण्डित युगबोध के साथ तालमेल बैठाते-बैठाते जीवन कितना खण्डित हो चुका है! मैं न चाहते हुए भी अतीत में लौटता रहता हूँ। शायद कुछ खो गया है जिसे फिर से पा लेने की उम्मीद छूटती नहीं। जब कभी घर जाता हूँ तो उन जगहों पर ज़रूर जाता हूँ जहाँ एकांत के क्षण बिताया करता था। जहाँ दुःख साझा करने के लिए मैदान की दूब थी, पत्थर की सीढ़ियाँ थीं। घर में एकांत कभी मयस्सर नहीं हुआ। न ही अब तक अपना कहा जाने लायक़ कोई कमरा है। एक खुली छत है जहाँ से खुला आकाश और खेत दिखता है। पतंगबाज़ी भी कितनी कम हो गई है अब। एक वक़्त था जब मोहल्ले का आकाश रंग-बिरंगी पतंगों से पटा रहता था। पतंग कटती और बच्चे हवा में लुढ़कती पतंग की दिशा में दौड़ लगाते। अब तो आकाश में कोई खेल नहीं होता। एक खेल होता है अब भी, चुनावी मौसम में। जब हेलीकॉप्टर अपने शोर के साथ मासूम पंछियों को डराते हुए आकाश से गुज़रता है।
शहर में, एक दरवाज़ा खुलता है आपके आतिथ्य में। यह शहर का स्वभाव है। एक वक़्त था जब गाँव में, किसी दरवाज़े तक पहुँचने से पहले आप पूरे गाँव के अथिति हो जाते थे। गाँव का यह स्वभाव कंक्रीट के नीचे दब गया है अब। उत्तराखण्ड के कवि महेश चंद्र पुनेठा ने कितना वाजिब लिखा है—
“अब पहुँची हो सड़क तुम गाँव
जब पूरा गाँव शहर जा चुका है
सड़क मुस्करायी
सचमुच कितने भोले हो भाई
पत्थर-लकड़ी और खड़िया तो बची है न!”
'बिखरा-बिखरा, टूटा-टूटा : कुछ टुकड़े डायरी के - सभी भाग यहाँ पढ़ें'